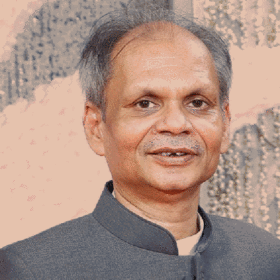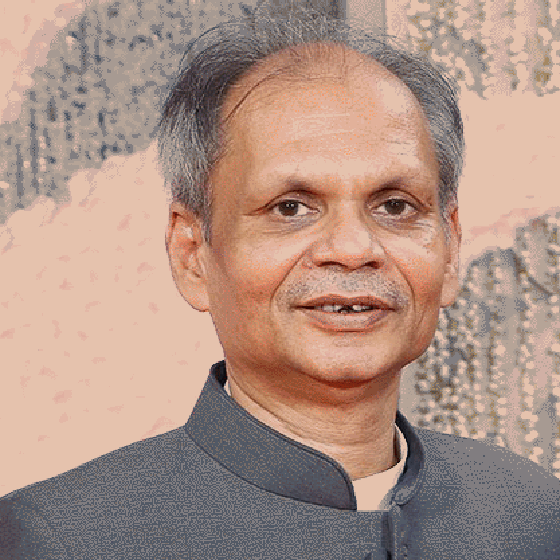हिंदुत्व की आध्यात्मिक एवं सामाजिक अवधारणा

१. जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दुओं की बहुलता के बावजूद हिन्दुत्व के दर्शन क्यों नहीं होते ? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा जटिल हैं।
२. इस्लाम, ईसाई तथा यहूदी जैसे व्यक्ति प्रवर्तित संप्रदायों के आसानी से समझ में आने वाले विश्वासों, जीवनमूल्यों एवं सिद्धान्तों के विपरीत हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों एवं विश्वासों को समझना आसान नहीं हैं । हिन्दू-धर्म के सिद्धान्त सूत्र रूप से लिखे होने की वजह से सर्व जन ग्राह्म नहीं हो सकते । प्रत्यक्ष में ऊपरी सतह पर जो अर्थ समझ में आते हैं वे मूल अर्थ से भिन्न हो सकते हैं अत: किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की सहायता से ही मूल अर्थ का ग्रहण संभव हो सकता है । बहुधा विरोधांभासी विचार भी दृष्टिगोचर होते हैं जिनका स्पष्टीकरण साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं । कोई भी एक धर्मग्रन्थ, एक विशेष लेखक, एक ऋषि मुनि अथवा एक विशेष ऐतिहासिक कालखण्ड, यहाँ तक कि कोई एक भौगोलिक परिवेश हिन्दू धर्म की उत्पत्ति एवं विकास का दावा नहीं कर सकता । विभिन्न भाषाभाषी विशाल जनसंख्या वाले विविधता से परिपूर्ण भारत की तरह ही यह हिन्दू धर्म समझने की दृष्टि से बड़ा जटिल, दुरूह एवं विराट है ।
३. अब हम बटवृक्ष की भाँति विराट हिन्दूधर्म को समझने का प्रयास करें। इस वृक्ष का मूल एवं मुख्य शाखा है बेद प्रतिपादित आचार संहिता । इसने सदियों से ही अतलांटिक महासागर से लेकर प्रशान्त महासागर तक, तथा मंगोलिया से लेकर दक्षिण के आस्ट्रेलिया एवं अफ्रिका तक के वृहद भू-भाग तक की विभिन संस्कृतियों एवं प्रजातियों के प्रभाव को अपने में समाहित किया है । इस प्रकार आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह यह विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है और इसमें इसने बड़ी
सफलता प्राप्त की है।
, ४. इतिहास के आदि काल से ही भारत में बाहर से लोगों के प्रवजन का सिलसिला जारी रहा । विभिन्न संस्कृतियों, धर्मो एवं भाषा के लोग आते रहे और यहाँ की विविधता में समाहित होते रहे । यह पता लगाना कि कौन लोग कब कहाँ से आए असंभव ही है । इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है । लेकिन परिणाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है | भारत की संस्कृति विभिन्न जातियों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का सफल समुच्चय है । इस समुच्चयी करण की प्रक्रिया का नाम ही ‘आर्यीकरण’ है । समय के प्रवाह
से उपासना, पूजापाठ, ध्यान आदि की पद्धतियों का समयानुकूल विकास हुआ । लेकिन मूल आधार हमेशा अपरिवर्तित ही रहा। इस प्रक्रिया का विकास प्रज्ञावान दूरदर्शी ऋषियों के अनुशासन में सम्भव हो सका | इसीलिए एक अव्यवस्थित, असंगठित धार्मिक व्यवस्था के बजाय जटिल होते हुए भी कलात्मक पतित्र रंगोली की भाँति सुन्दर एवं सुरुचिपूर्ण व्यवस्था के रूप में इसका विकास हुआ । जैसे अनेक राज्यों के संघ के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ है अथवा जिस प्रकार अनेक छोटी-बड़ी नदियों को समाहित करती हुई गंगा का प्रवाह है ।
५. इतिहास के आरोह अवरोह के क्रम ने दुर्भाग्य वश हिन्दुत्व की आत्मसात् करने की प्रवृत्ति एवं उदात्त भावना के दैवी उपहार का अपहरण कर लिया। सम्पूर्ण राष्ट्र की मानसिकता में परिवर्तन हुआ, परिस्थितियों के कारण हम भारतवासी अन््तर्मुखी बन गए । हमने वाह्म आक्रमणों के प्रति सुरक्षात्मक ‘ नीति अपनाई तथा यदि सम्पूर्ण का बचाव न कर पाएं तो कम महत्व के
अंश का त्याग कर अवशिष्ट महत्वपूर्ण अंश का ही बचाव किया जाय की नीति अपनाई । रीति रिवाजों में जो लचीलापन था, जिसके कारण हम औरों को समाहित कर पाते थे, उनमें भी बाध्य होकर संकीर्णता का समावेश करना पड़ा। सामाजिक दायरे से निष्कासन की प्रक्रिया तो सहज थी लेकिन पुनरागमन की प्रक्रिया ही नहीं हुई अपितु परावर्तन के दरवाजे बन्द ही कर दिये गये । तीर्थयात्रा के अतिरिक्त भ्रमण पर भी रोक लगाई गई, समुद्री यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाए गए, अन्य धार्मिक समुदायों एवं जातियों से आसानी से मिलने-जुलने तथा अन्तर्जातीय विवाहों को हतोत्साहित किया गया । समाज के सुसंगठित अस्तित्व को बचाए रखने के लिये बिखरे हुए ढीले ढाले सामाजिक ढाँचे के बजाय सुसम्बद्ध छोटी इकाइयों को वरीयता दी गई । जब हिन्दू समाज संकट के घेरे में आबद्ध हुआ तब अपनी सुरक्षा के लिए उपरोक्त उपाय किए गए । तत्कालीन परिस्थितियों की बाध्यता
। के कारण सामाजिक संगठन एवं पवित्रता को बनाए रखने के लिये उठाये ये कदम उचित थे लेकिन परिस्थितियों के बदलाव के बाद भी हम उन्हीं रढ़ियों से चिपके हुए हैं यही इतिहास की विडंबना है ! आज भी हम सुरक्षात्मक एवं होन मानसिकता के वातावरण से उबर पाने में अक्षम हो रहे हैं।
६. हिन्दूधर्म के चिन्तन का मूल आधार समग्रता का है चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा भौगोलिक स्तर पर ही क्यों न हो । लेकिन वर्तमान काल में हमने इस समग्रता के विचार को तिलांजलि दे दी और हम जाति, समाज, संघ, सम्प्रदाय के संकीर्ण दायरों में फँस गए और हिन्दू धर्म को इन सबका ही समुच्चय बना दिया जो कि एकता के प्रतीक के अभाव में बिखराव एवं रुढ़िवादिता का प्रतीक बन कर रह गया । इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आए । राजनीति के लोकतनत्रीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों ने अपने निहित क्षुद्र स्वार्थ के लिए विभिन्न सामाजिक घटकों में और अधिक अलगाव की भावना भरनी प्रारम्भ की । उन घटकों को यह समझाया गया कि इसी अलगाव से ही वे अपना अस्तित्व बचाने में सक्षम हो सकेंगे। हिन्दू समाज के इस विभाजन ने राष्ट्र विरोधी तत्वों को यह कहने का अवसर प्रदान कर दिया कि अभिज्ञेय हिन्दू बहुमत के अभाव
में भारत बस्तुत: अल्पमत वालों का राष्ट्र है । चूंकि सत्य ही चिरस्थायी होता है और हिन्दुत्व का सत्य उसकी अन्तर्निहित एकता है अतः यह मिथ्या प्रचार कालक्रम से निश्चय ही समाप्त हो जाएगा ।
७. हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये कि आधुनिक सन्दर्भ में हिन्दुत्व अनावश्यक भार से बोझिल हो रहा है अत: उसे समानुपातिक एवं सन्तुलित रूप देने के लिये समय के प्रतिकूल तत्वों का परित्याग करना आवश्यक है । हिन्दुत्व को संकोर्णता का परित्याग करते हुए उसे अन्तरराष्ट्रीय एवं सर्वदेशीय रूप देना चाहिये । अपनी सुरक्षा के लिये केवल सुरक्षात्मक ही
नहीं आक्रामक शक्ति सम्पन्न बलिष्ठ, मजबूत एवं संसक्तिशील होना आवश्यक है ।
८. हम इस प्रकार के बलिष्ठ सौष्ठव को कैसे प्राप्त करें ? इसके लिये आवश्यक है जो कमजोर अवयव हैं उन्हें व्यायाम द्वारा पुष्ट करें, उनकी समुचित देख-भाल सेवा करें तथा अनावश्यक अशुद्धियों का विचार पूर्वक करें एवं विस्तार तथा संकोचन के द्वारा शरीर को क्रियात्मक तनाव प्रदान करें । हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत एवं पूर्वजों का स्मरण करते हुए अपने मूल का संरक्षण तथा स्मरण करते हुए विकृत किए गये इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिये । यह कार्य कठिन है लेकिच असंभव नहीं ।
९. हिन्दू धर्म को सनातन धर्म कहा गया है जिसका न आदि है न अन्त । वस्तुत: यह शाश्वत धर्म है । इस धर्म का न तो कोई एक प्रवर्तक है, न कोई एक विशिष्ट धर्मग्रन्थ है, न कोई एक संस्थापक । मानव की आध्यात्मिक अन्वेषण की प्रवृत्ति का पर्यायवाची है सनातन धर्म । प्रज्ञावान ऋषियों ने समाधि अवस्था में मन्त्रों के दर्शन किए और उनके द्वारा गाए गये मंत्रों को महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया तथा अपौरुषेय बैदिक मंत्रों का वर्गीकरण किया। उन्होंने ब्रह्म के एक अथवा अनेक रूपों, सगुण एवं निर्गुण स्वरूपों, देव एवं दैत्य कुलों, लोकोत्तर प्राणियों तथा पवित्रात्माओं का विस्तार से वर्णन किया । हम इनका आवाहन कर सकते हैं और आबाहित देवताओं को विसर्जित कर सकते हैं, उनकी सहायता एवं सहयोग की आकांक्ष करते हैं और उसके बदले में उनकी पुष्टि के लिये जो विहित कर्म बनाये गये हैं वे भी सम्पन्न करते हैं । ये देवता भी हमारी ही तरह इस अखिल ब्रह्माण्ड के अभिन्न अंग हैं । उन्हें हमारे स्तर पर लाने एवं हमारे बीच अवतरण कराने के लिए ध्यान की अपरिहार्यता बताई गई है । ध्यान से ही हम इस लोक का मानसिक रूप से अतिक्रमण करने में सक्षम हो सकते हैं । मानव एवं देवताओं का यह सम्मिश्रण इस ब्रह्माण्डीय रंग मंच में उन्हें तथा हमें एक दूसरे का सहभागी बनाता है ।
१०. सनातन हिन्दू धर्म की यह अवधारणा है कि इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से हुई है और वह ब्रह्म ही इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गया । यह सृष्टि अनादि है, जो अनादि है उसका अन्त संभव नहीं। काल के दृश्य पटल पर यह सृष्टि सुव्यवस्थित तरीके से ब्रह्म से व्यक्त होती है और ब्रह्म में ही उसी प्रकार लीन हो जाती है जैसे मकड़ी से जाला । परमतत्त्व ही अपने को विभिन्न नामों, रूपों, गुणों एवं क्रियाओं में दृश्य एवं अदृश्य रूप से न केवल इस पृथ्वी पर अपितु विराट ब्रह्माण्ड के| लोकों में प्रकट करता है । सुव्यवस्थित आरोह अवरोह, सक्रियता एवं विश्राम की अवधि से संयुक्त एक चक्र की समाप्ति के पश्चात् दूसरे चक्र का प्रारम्भ होता है । बोध के एक स्तर पर यह प्रक्रिया बड़ी विशाल, गोचर एवं विस्मयकारी है वहीं दूसरे स्तर पर वह सत्य की मानसिक़ संकल्प जनित रचना है । सृष्टि रचना इतनी जटिल है कि इसमें एक जगत के अन्दर छोटे बड़े दृश्य-अदृश्य अनन्त जगत समाहित हैं जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती और इनको पूरी तरह समझ पाना असंभव है ।
११. स्थूल एवं सूक्ष्म जगत (पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड) उस एक ही तत्व के अभिन्न अंग है । दोनों ही स्तरों पर इनमें अद्भुत सामंजस्य है । जगत की सृष्टि का कार्य कारण का विधान अत्यन्त सरल एवं सुरुचिपूर्ण है । यह विधान वृहद् और जटिल होने पर भी बोधगम्य है तथा विभिन्न स्तरों पर सक्रिय है । निष्कर्ष है कि इसका स्वरूप आध्यात्मिक है इसी के कारण व्यक्त अथवा अव्यक्त का स्वरूप भी आध्यात्मिक ही है । यह ऋत है जो उत्पत्ति, पालन एवं संहार का नियमन करता है।
१२. इस उत्पत्ति एवं संहार के ब्रह्माण्डीय अधिनियम का आधार है ‘कर्म’ कार्य- कारण, क्रिया-प्रतिक्रिया, बीज और फल, “जो जैसा बोवे बैसा काटे” । यह सिद्धान्त अपरिवर्तनीय, अकाट्य एवं अटल है । इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को कर्म करने की स्वतन्त्रता है तथा तदनुरूप कर्मफल प्राप्त करने की आश्वस्ति । कर्म एवं कर्मफल का अपरिहार्य सम्बन्ध इतना पेचीदा भी है कि कभी कभी इसको समझना दुरूह हो जाता है । कर्म एवं कर्मफल का सिद्धान्त न केवल व्यक्ति विशेष को अनुशासित करना है अपितु परिवार, राष्ट्र और यहाँ तक कि मानव इतिहास की धारा को भी प्रभावित एवं अनुप्राणित करता है । हम भविष्य के निर्माता भी हैं लेकिन साथ ही साथ हम अपने अतीत से बंधे हुए भी हैं । यह उभयमार्गी दन्द्वात्मक प्रक्रिया है । हमारे भूत काल के कर्म हमारे वर्तमान के अनुशास्ता हैं और वर्तमान के कर्म भविष्य के नियामक हैं ।
१३. प्रत्येक प्राणी को जीवन के अनेक स्तरों पर कर्म फल सिद्धान्त का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । यह सिद्धान्त आध्यात्मिक है अत: कर्मफल का निरूपण भी आध्यात्मिक आधार पर ही हो सकता है । कर्मफल का भोग किये बिना समाप्त नहीं होते और यह आवश्यक नहीं कि पिछले जन्म का कर्मफल भोग केवल एक ही जन्म में समाप्त हो जाय । इसके लिये अनेक जन्मों की यात्रा भी करनी पड़ सकती है । जब कर्मफल भोग शून्य हो जाते हैं तभी मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है ।
१४. हिन्दू धर्म अन्तर एवं वाह्य दोनों स्तरों पर कर्म सिद्धान्त की अवधारणा को मान्यता प्रदान करता है । जीव के कर्मों के अनुसार अनेक लोकों की अवधारणा की गई है। उन लोकों में रहने वालों की सामर्थ्य तथा अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन है । देवता, यक्ष, गंधर्व, पितर, राक्षस, असुर, भूत, पिशाच आदि के उच्च एवं निम्न श्रेणी के अनेक लोक हैं । इन लोकों में रहनेवाले ये देवता, यक्ष, गंर्धव आदि अपने पूर्व कृत कर्मों के अनुरूप फल का भोग करते हैं । जिस प्रकार हमारा शरीर पाँच भौतिक तत्वों (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा-पंच रचित यह अधम शरीरा) से बना है उसी प्रकार उनका शरीर हमसे भिन्न तत्वों से निर्मित है और उसी देह में वे अपने कर्मफल का भोग करते हैं । यह तो बात हुई बाह्य स्तर की । अब हम अन्तर स्तर की चर्चा करते हैं | कर्मफल का सिद्धान्त अन्त:तल स्तर पर भी उतना ही प्रभावी है । स्वर्ग एवं नरक कहीं बाहर नहीं अपितु हमारे अन्दर ही हैं । हम अपने ही कमों एवं विचारों से स्वर्ग एवं नरक का निर्माण करते हैं । कुछ लोग स्वनिर्मित नरक में रहते हैं वहीं दूसरी ओर शुद्ध सात्विक विचारों के अनुरूप सत्कर्म करते हुए कुछ लोग आन्तरिक आनन्द की अनुभूति करते हुए स्वर्गीय सुख का उपभोग करते हैं | समय समय पर हमारे मन के विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं | भगवद् भक्त जिस परमानन्द
का अनुभव करते हैं वह अनिवर्चनीय, अकथनीय एवं अखण्ड आनन्द है।
१५. हिन्दू धर्म के निम्नलिखित पाँच सूत्र हैं :-
- १. यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे. : जो स्थूल देह (पिण्ड) में है उसीका बृहद् रूप ब्रह्माण्ड में है ।
- २. कर्म कर्मान्तर | भोक्तव्यं कृत॑ कर्मशुभाशुभम् ।
- ३. जन्म जन्मान्तर : “पुनरपि जनम पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननी जठरे शयनम् ।’ (पुनर्जन्म का सिद्धान्त)
- ४. चित्त चित्तान्तर : विचारों के उदात्त से लेकर लौकिक तक विभिन्न स्तर
- ५. लोक लोकान्तर : अस्तित्व की निविधता एवं व्यापक आयाम
१६. बौद्ध एवं जैन दर्शन सहित सभी भारतीय मतों में उपरोक्त पाँचों सूत्र सर्वमान्य हैं । विराट हिन्दू धर्म की ही प्रशाखा के रूप में माने जाने वाले बौद्ध एवं जैन मत, हिन्दू धर्म से अनेक मायनों में भिन्न होते हुए भी उपर्युक्त पाँचों सूत्रों को अपने सिद्धान्तों में समाहित किये हुए हैं ।
१७. हिन्दूधर्म का अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विकास हुआ । इसके आध्यात्मिक सिद्धान्त सर्वांग सम्यक् एवं बोधगम्य हैं लेकिन अपनी अपनी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक क्षमता के अनुरूप सिद्धान्तों की व्याख्या करने में सभी स्वतत हैं। इसीलिये यह कह गया है – ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति” एक ही सत्य की व्याख्या भिन्न-भिन्न मनीषी अपने अपने तरीके से करते हैं ।