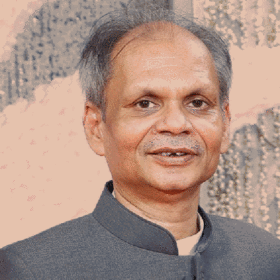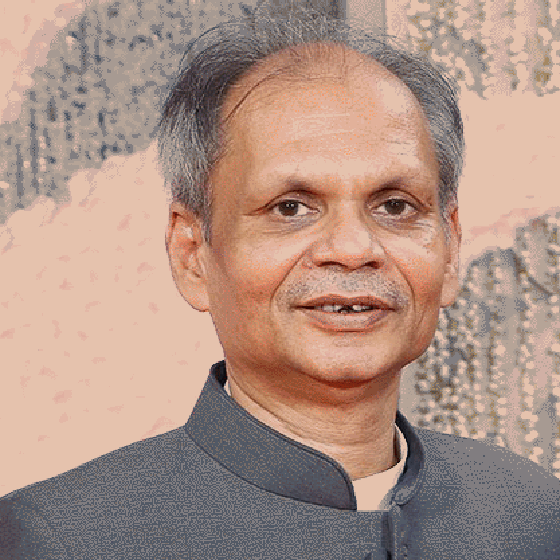हिंदुत्व की आध्यात्मिक एवं सामाजिक अवधारणा Part 2

१८. हिन्दू धर्म के एकत्व एवं अनेकत्व के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करें । संकीर्ण, ऐकान्तिक एवं परिभाषित मुस्लिम, ईसाई तथा यहूदी धर्मों को समझना आसान है । इन धर्मों में भी अनेक सम्प्रदाय, विभाग एवं मुट है लेकिन वे इतने सुस्पष्ट नहीं हैं कि उनके अनुयायियों की पहचान को वे प्रभावित कर सके । लेकिन हिन्दू धर्म में यह स्थिति नहीं है ।
१९. हिन्दू धर्म के सम्प्रदायों में समरसता अथवा एकरूपता के अभाव को समझने के लिये इसकी विकास यात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है । एक ही धर्मग्रन्थ, एक ही मसीहा की मान्यता वाले प्रवर्तक धर्म के उद्भव के पूर्व २०० वर्षों में उपासना, कर्मकाण्ड तथा आध्यात्मिक जिज्ञासा सभी व्यक्तिगत साधना तक सीमित थे अथवा एक सम्प्रदाय विशेष तक सीमित थे । विशेष प्रकार की उपासना अथवा मत का विकास एक सिद्ध, ब्रह्मज्ञानी आचार्य के उपदेशों के अनुरूप-आचार्य के व्यक्तित्व एवं साधना के प्रभाव
से होता था | ऐसे आचार्य अपने शिष्यों की अलग पहचान के निमित्त एक निश्चित प्रकार की पूजा पद्धति, वस्त्र निर्धारण, कर्मकाण्ड, कुछ विशेर्ष धर्म ग्रन्थ, विशेष देवी देवता की पूजा का विधान करते थे । इन्हीं अनुयावियों के कारण कालक्रम से सम्प्रदायों का विकास हुआ जो कालान्तर में अपनी अलग पहचान से जाने गए लेकिन बे सम्प्रदाय विराट हिन्दू धर्म के ही
अभिन्न अविछेद्य अंग बने रहे ।
२०. सम्परदायों का इस तरह का विकास हिन्दू धर्म की आधारभूत दार्शनिक मान्यताओं के कारण संभव हो सका । मान्यताओं के आधारभूत एकत्व को सुरक्षित रखते हुए, वेदों की अपौरुषेयता एवं वरिष्ठता को स्वीकारते हुए, सृष्टि की संरचना में परमतत्व की, कर्मसिद्धान्त एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त आदि की मान्यता को आधार मानने के पश्चात हिन्दू धर्म ने अन्य मान्यताओं एवं सिद्धान्तों की व्याख्या में सम्प्रदायों को पूरी स्वतन्त्रता दे । रखी है । प्रत्येक व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय अपनी अपनी रुचि एवं क्षमता के है अनुरूप उपास्य, उपासना पद्धति एवं साधना के मार्ग का चुनाव करने में स्वतन्र है । वर्तमान युग में जिस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं के चयन का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है उसी प्रकार हिन्दू धर्म में आध्यात्मिक का व्यापक क्षेत्र है जिसमें साधक अपनी रूचि, क्षमता एवं स्वभाव के अनुरूप साधना पद्धति का चुनाव कर सकता है ।
२१. इन्हीं उपरोक्त कारणों से हिन्दू धर्म में अनेक सन्त महात्माओं, प्रज्ञावान महापुरुषों, साधकों द्वारा अनुभूत तथा आर्ष ग्रन्थों द्वारा अनुमोदित अनेकानेक चकित एवं विस्मित करने वाले सिद्धान्त एवं उपासना कौ पद्धतियां पाई है जाती है । यहाँ तक कि जिन्होंने सांसारिक भोग विलास का त्याग करके सन्यास ले लिया है उनके भी भिन्न भिन्न सम्प्रदाय, आम्नाय मठ आदि होते
हैं | गृहस्थों का भी जाति, उपजाति, व्यवसाय, सम्प्रदाय, उपसम्पदाय, भाषा आदि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है । यह वर्गीकरण बहुभाषी एवं अनेकानेक सम्प्रदायों की सीमा का अतिक्रमण करते हुए अनेकता में एकता की प्रतिष्ठा करता है ।
२२. सदियों पूर्व भारत के लोग दीर्घकाल तक बड़ी शान्तिपूर्वक रहे इसीलिये सब सम्प्रदाय बड़ी समृद्ध परम्परा से पृष्पित एवं पल्लवित होते रहे तथा इससे एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगत जीवन शैली का विकास हुआ ।
२३. किसी ने भी – न तो विद्वानों ने, न ही जनगणना विभाग ने इन अनगिनत ‘सम्मदायों की गणना की लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य से अभिज्ञ है कि ये सम्प्रदाय अनगिनत है और उनकी संख्या आज भी बढ़ती ही जा रही है। इसके बावजूद इस अनेकता में एकता के सूत्र विद्यमान है । ये केन्द्राभिसारी एकत्व के सूत्र केन्द्रापसारी शक्तियों को पराभूत करते रहते हैं । ऐसे ही एकता के सूत्र हमारे गौरवशाली इतिहास में भी अनुस्यूत हैं ।
२४. हमारे इतिहास की काल यात्रा के इस जटिल घटना क्रम को जिस एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है वह है – ‘आर्यीकरण” । भारतीय आर्य सभ्यता के इस विश्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त इस सभ्यता ने देवभाषा संस्कृत में दर्शन, सर्व जन हिताय उदात्त विचारों एवं सुसंस्कृत तथा अनुशासित जीवन शैली के सूत्रों को व्यक्त किया है । विश्व समुदाय की वेदों के प्रति
आदरणीय अवधारणा के समान इन उपरोक्त उदात्त विचारों की संवाहक ४ संस्कृत भाषा भी सभी सम्म्रदायों द्वारा प्रतिष्ठित, गृहीत एवं आदरणीय है ।
२५. अब हम हिन्दू धर्म की निम्नलिखित दस मूल अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें :
- ईश्वर – परमात्मा,
- पाप – पुण्य
- आत्मा – जीवात्मा
- अविद्या – विद्या
- उपासना
- अवतार
- देवता
- वर्णश्रम
- मोक्ष
- संस्कार
२६. हिन्दू धर्म का आधार अत्यन्त व्यापक है जिनमें से कुछ मुख्य सूत्रों का चुनाव किया गया है । ये सूत्र हिन्दू धर्म की मूल प्रकृति की एक झलक प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, जिसके जटिल एवं दुरूह से लगने वाले सिद्धान्त हिन्दूधर्म को एक सच्चे तथा मानवता को शाश्वत आध्यात्मिक अनुशासन एवं पथप्रदर्शन करने वाली भव्यता प्रदान करते हैं | एक ही मजहबी ग्रन्थ तंथा एक ही पैगम्बर को माननेवाले व्यक्ति प्रवर्तित धर्मों के आगमन के पूर्व तक यही एक सनातन हिन्दू धर्म विश्व को समुचित आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने वाला था । ये संकीर्ण सिद्धान्तों वाले प्रवर्तक धर्म अधिक समय तक टिकने वाले नहीं है । भविष्य में तो सहिष्णु, तर्क बुद्धि परक (]२४४07४7॥४७() समयानुकूल विचारों को ग्रहण करने वाला सनातन धर्म ही विश्व के समस्त मानव समुदाय की सर्वांगीण उन्नति के मार्ग दर्शन करने में सक्षम होगा ।
२७. अब हम ईश्वर’ की अवधारणा से चिन्तन प्रारम्भ करें । हिन्दू धर्म में ईश्वर तत्व न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग ( न त्वं स्त्री न पुमान न कुमार उतवा कुमारी) न तो यह पृथ्वीलोक से इतर किसी काल्पनिक स्वर्गलोक में वास करने वाला है और न ही पृथ्वी के किसी एक भाग का वासी है, न यह देवताओं अथवा अप्सराओं के मध्य रहनेवाला है और न ही असुरों के मध्य। अपितु ईश्वर अथवा ब्रह्म नाम, रूप आकार रहित अपरिच्छिन्न तत्व है । यह अखिल ब्रह्माण्ड का अधिष्ठान है । यह तत्व इन्द्रियातीत, अज्ञेय है ।
श्रीमद् भगवदगीता में भी इस तत्व का रूपकों के माध्यम से वर्णन किया गया है । प्राचीन ऋषियों एवं सन्त महात्माओं ने अनेकों प्रकार से उस तत्व की महिमा का अपने अपने अनुभवों के आधार पर वर्णन किया है । ईश्वर तत्व ही हिन्दू धर्म का मूल आधार है । इसी अव्यक्त तत्व के साहचर्य से ही व्यक्त यह जड़ सृष्टि भी सत्य, पवित्र एवं ईश्वरत्व से अनुप्राणित होती दिखाई देती है । प्रकृति के संयोग से ही परम तत्व द्वारा उत्पत्ति, पालन एवं संहार का कार्य सम्पन्न होता रहता है ।
२८. अब हम आत्मा जीवात्मा पर चर्चा करेंगे । आत्म तत्व जब स्थूल शरीर से परिच्छिन हो जाता है तब इसे जीवात्मा कहते हैं । यह जीवात्मा आत्मत्त्व का अभिन्न अंश है । जिस प्रकार आत्म तत्व शाश्वत है, नित्य है उसी प्रकार यह आत्मा भी शाश्वत एवं नित्य है । स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता । स्थूल शरीर से तादात्म्य होने पर वह कर्मों का भोक््ता हो जाता है । जीवन की एक यात्रा की समाप्ति के बाद यह जीवात्मा पुनः दूसरे शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी यात्रा जारी रखता है ।
जब व्यक्ति को साधना के द्वारा नाम रूपात्मक दृश्य जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है उस समय द्वैत बुद्धि के नष्ट होनेपर जीव ब्रहैक्य का बोध होता है तब व्यक्ति जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है । आत्म स्वरूप के बोध होने पर पुरानी बासनाओं का क्षय हो जाता है तथा नई वासनाओं के निर्माण के अभाव में पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। यह स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य के कर्म दिक् काल सापेक्ष हैं वहीं आत्मा की यात्रा आध्यात्मिक क्षेत्र में होती है ।
२९. उपासना अर्थात् पूजा की पद्धति एवं प्रकार, दूसरा विचारणीय विषय है, हिन्दू धर्म-इस्लामी मजहब के कलमा अथवा नमाज की भाँति अनन्य मानकी कृत पद्धति का प्रावधान नहीं करता । इसके लिये सबसे पहले अपनी रूचि एवं क्षमता के अनुरूप सम्प्रदाय का चुनाव करने के पश्चात उसी अनुरूप उपासना पद्धति का निर्द्धारण किया जाता है । इसके बावजूद साधक उपासना
पद्धति में परिवर्तन करने के लिए स्वतन्त्र होता है । इस चुनाव में कहीं कोई बाध्यता अथवा अपने मत विशेष को बलात थोपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । प्रत्येक साधना एवं उपासना पद्धति अपने में सर्वाड़् पूर्ण है । गीता का कथन है –
ये का मां अपडनते तांस्तधैव भजाग्यहम् /
मगर वत्मचिवर्तनते मजुष्या: पार्थ सर्व: //
मुझे जैसे भजते हैं, मैं उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूँ । हे पार्थ ! सभी मनुष्य सब प्रकार से, मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं ।
स॒ कया श्रद्धया इक््तस्तस्वाराधन मीहते /
लगते च तत: काम्रानयवैव विहितानितान् ।/
वह (भक्त) श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किये हुए इच्छित भोगों को नि:सन्देह प्राप्त करता है । हिन्दू धर्म की इस विशाल आध्यात्मिक प्रयोगशाला में प्रत्येक प्रकार की यहाँ तक कि तामसी प्रकृति के लोगों के लिए घृणास्पद, वीभत्स, बेतुकी सी दीखने वाली कौलिक उपासना पद्धतियाँ (भूत प्रेत आदि की) भी विद्यमान है । व्यक्ति अपनी श्रद्धा, विश्वास, क्षमता, रुचि, स्वभाव के आधार पर उनमें से अपने अनुरूप उपासना पंद्धति का चुनाव करने में स्वतन्त्र है ।
३०. अब हमारी अगली अवधारणा का विषय है देवता । हिन्दू धर्म का विदेशी लोगों ने इसके विभिन्न रंग, वर्ण, एवं आकृति के असंख्य देवी देवताओं के स्वरूपों एवं प्रतीकों के अज्ञान के फलस्वरूप इसे बहुदेववादी, आदिम, अशिष्ट धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है । हिन्दू धर्म की विभिन्न पूजा पद्धतियों- जिनमें सात्विक पूजा पद्धति से वृक्षों, सर्पों, भूत प्रेतों तक की तथा तान्रिक पद्धति, ऐसे कर्मकाण्ड जिनमें नर बलि, नग्न नृत्य, सुरा, मत्स्य, माँस, मद्य आदि शामिल हैं, का भी समावेश है । ऐसे चित्र विचित्र
धर्म को सामी जगत (5९7४४८ ४०९५) के एक लीक पर चलने वाले धर्मावलम्बियों के लिये समझना दुष्कर है । हिन्दू धर्म अपने में जीवन के सम्पूर्ण एवं विरुपता के साथ समग्र रूप में स्वीकार करता है । हिन्दू धर्म का जीवन दर्शन वाह्म सौन्दर्य से अधिक आन्तरिक सौष्ठव पर अधिक बल देता है । फ्रायड सहित अन्य पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी मन एवं प्राण शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन एवं चित्रण करने में असमर्थ रहे हैं । आदिम मानव के अश्मीभूत समाज के सादृश्य खोजनेवाले मानव शास्त्र के मानक के आधार पर मन एवं बुद्धि की खोज असंभव है । शोधकर्ताओं के प्रयास से मिथक, जादू टोने, मंत्र एवं मंडल जन्तर (ताबीज) एवं झाड़फूंक (अभिचार) आदि के बारे में अभिज्ञता बढ़ी है । बौद्ध तंत्र के साध्यम से इस दृश्य जगत से इतर जगत के अपार्थिव प्राणियों जैसे देवता, राक्षस, प्रेतआदि भी ज्ञान की परिधि में आने लगे हैं । ये देवता आदि हमारी तरह पंचभौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है अपितु इनकी निर्मिति तेजस् आदि तत्वों से है तथा हमारी व्यक्तिगत आकांक्षा के अनुरूप इनकी कल्पना की जाती है।
३१. हमारा अगला विषय है मोक्ष – मोक्ष के विषय में आम लोगों में बड़ी भ्रान्त धारणा है। मोक्ष पलायनवाद का नाम नहीं है न ही यह एक नकारात्मक अवधारणा है । मोक्ष एक पूर्णत: सकारात्मक अवधारणा है । आंग्ल भाषा में इसका समानार्थी कोई शब्द नहीं है । उद्धार (2९एश’८९) अथवा मुक्ति (/90/2४07/) जैसे शब्द मोक्ष का वास्तविक अर्थ प्रकाशित करने में सर्वथा अक्षम हैं । जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होता है, जब स्व॒ के विषय में अज्ञान का आवरण नष्ट होता है तब उस ज्ञान के कारण उसे आत्म साक्षात्कार होता है और साधक को शाश्वत आनन्द की अनुभूति होती है, ऐसी अवस्था ही मोक्ष की अवस्था कही गई है । तब उस साधक के जीवन में दिव्यता, शुचिता, पवित्रता एवं सुगन्ध का प्रवेश हो जाता है यही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति का प्रमाण है । ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त साधक को उस अवस्था में साधना की आवश्यकता नहीं होती, साधक आप्त काम हो जाता है, साधक अपने को समग्रता से अभेद का अनुभव करता है । आत्म बोध की यही अवस्था गौतम बुद्ध को बोधिवृक्ष के नीचे प्राप्त हुई । ऐसे ही साधकों को जीवनमुक्त कहते हैं । प्रवर्तक धर्मों के विपरीत हिन्दू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक मानव को है ।
३२. मानव जीवन के केन्द्र में पाप पृण्य की अवधारणा का मुख्य स्थान है । हमारे कर्म की पहचान का यही आधार है कि वे हमें कहाँ ले जाते हैं पाप की ओर या पुण्य की ओर । कर्मफल का अकाट्य सिद्धान्त हमें प्रत्येक क्षण सावधान सचेत एवं उत्तरदायी बनाता है । लेकिन कर्मफल के सिद्धान्त को समझना इतना आसान नहीं है । (किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता: गीता) हिन्दू धर्म में कर्म के अच्छे बुरे का सहज बोधगम्य निश्चित मानक नहीं है । तथापि कर्म की पृष्ठ भूमि में कर्म किस उद्देश्य से किया जा रहा है, अथवा व्यक्ति की भावना क्या है – इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। आमतौर पर आत्मोद्धार की आकांक्षा न करने वाले प्रेय कामी व्यक्ति के सकाम कर्म बन्धन कारक (जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाले) होते हैं। कारण वे क़र्म वासना, इच्छा, लोभ, काम, क्रोध, धनलोलुपता, ईर्ष्या आदि से अनुप्राणित होते हैं । गीता का कथन है कि यदि साधक काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह कर्म बन्धन कारक नहीं होता । अत: हिन्दू धर्म की अवधारणा के अनुसार जो कर्म अज्ञान से प्रेरित होकर सकाम भावना से किये जाते हैं, वे ही बन्धन कारक होते हैं तथा जो कर्म हमें आध्यात्मिकता से दूर ले जाने वाले होते हैं- बे कर्म ही पाप की श्रेणी में आते हैं, अन्य कर्म नहीं ।
३३. अब हमें अविद्या के बारे में जानना चाहिये कि ‘अविद्या’ क्या है ? अपने स्वरूप के प्रति अनभिज्ञता अपने को मूल चेतन तत्व से भिन्न मानते हुए देहात्म भाव में रहना ही अविद्या है । देह्ात्म भाव में रहते हुए वासना, इच्छा, काम, क्रोध से प्रेरितकर्म कर्मफल के बन्धन में बाँधने वाले होते हैं । हिन्दू धर्म द्वारा निर्दिष्ट साधना पद्धति से मनुष्य का अविद्या का आवरण हट जाता है तभी वह अपने स्वरूप के प्रति अभि्ञता प्राप्त कर सर्वाड़ सुन्दर व्यक्तित्व ह को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है । साधना के द्वारा अविद्या के नाश के उपरान्त आत्म साक्षात्कर प्राप्त व्यक्ति ही जीवन-मुक्त कहलाता है ।
३४. अवतार क्या है ? ब्रह्म के एक अंश का सीमित लक्ष्य एवं सीमित अवधि के लिये किसी भी रूप में इस भू लोक पर अवतरण ही अवतार है | विकासवाद के लिए भी यह अत्यावश्यक है । उद्धार के लिए अवतरण की आवश्यकता क्यों ? इसके लिए गीता का वचन है –
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत ।
अध्ुत्यानम्रधर्मस्व तवात्यानं स॒जास्यहम् //
है भारत ! जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ ।परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्क्रताम् /
बर्म संस्थापनार्धाव संभवामि गये गे //
साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापन के ‘ लिये मैं युग-युग में प्रकट होता हूँ । केवल घटनाओं का इतिवृत्त ही नहीं है । हिन्दू धर्म ऐसे इतिहास को निरर्थक मानता है । आध्यात्मिक क्षेत्र में आवर्ती प्रक्रिया (0एलांट्वा [700९७७) अवतरण की प्रक्रिया अन्तर्निहित है । इसीलिए प्रत्येक युग, महायुग, मन्वन्तर एवं कल्प में ईश्वर के अवतार हुए हैं । हम लोग भगवान के अवतरण से लाभान्वित होते हैं – शायद भगवान भी अवतरण काल में भक्तों का सान्निध्य पाकर आनन्दित होते हैं।
३५. ‘“वर्णाश्रम’ व्यवस्था हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की आधार शिला है । वर्णाश्रम शब्द “वर्ण” एवं आश्रम” से मिल कर बना है । दोनों में परस्पर सम्बन्ध होते हुए भी अकाटय एवं अभेद्य सम्बन्ध नहीं है । इन शब्दों में आध्यात्मिक सत्य एवं अवधारणा संनिहित है अत: इन शब्दों की व्याख्या तदनुसार ही होनी चाहिए । समाज में कार्य के सम्यक् क्रियान्वयन एवं संचालन के लिये ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र इन चार वर्णों की संकल्पना की गई है । यह व्यवस्था निन्दा मूलक यानि छोटे बड़े की असमानता की सृष्टि के दृष्टिकोण से नहीं की गई है । यदि इस व्यवस्था का सही पर्यवेक्षण यानि आध्यात्मिक निरीक्षण करें तो पायेंगे कि समाज की आधुनिक आवश्यकताओं की सम्यक् पूर्ति इस व्यवस्था के सुसंचालन से हो सकती है । गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है –
चाहुर्वर्ण्य ग्रया सृष्ट गुण कर्म विभायग्: / तस्य कर्तारपि मां विदृध्य कतरिमवन्यदम् // ४-१३
गुण एवं कर्मों के विभाग से चातुर्व्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है । यद्चपि मैं उसका कर्ता हूँ तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो । तब फिर विरोधाभास की गुंजाइश कहाँ है । आजकल यह आरोप लगाया जाता है कि ‘क्या ब्राह्मणों को समाज में विशेषाधिकार नहीं दिया गया है ? समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों के सम्यक संचालन की दृष्टि से गुण (सत्व, रज एवं तम) तथा कर्म के आधार पर वृत्ति मूलक वर्गीकरण किया गया है । यह व्यवस्था जन्मना नहीं, कर्म के आधार पर है । बलात् लादी नहीं गई है अपितु स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है । इस व्यवस्था का आधार स्वाभाविक है अध्यारोपित नहीं । इस व्यवस्था के निषेधात्मक पक्षों को भी जानना चाहिये । वर्ण व्यवस्था में जन्म एवं अर्थ के आधार पर ऊँच नीच की भावना एवं उद्धतता नहीं है । व्यवस्था आदेशात्मक नहीं अपितु विवरणात्मक है । इस व्यवस्था में जड़ता नहीं लचीलापन है। अस्पृश्यता के अभिशाप से युक्त जातिवाद का कहीं भी समर्थन नहीं किया गया है । कालचक्र से इस वैज्ञानिक व्यवस्था में जो विकृतियाँ आई है उनका निराकरण करने की आवश्यकता है न कि व्यवस्था को ही तिलांजलि देने की । हमारे जीवनक्रम में भी हम इन चारों स्तरों से गुजरते हैं । शुद्धीकरण के लिये किये गए शास्त्र विहित संस्कारों से संस्कारित किये जाने के पूर्व हम जन्म से शूद्र ही होते हैं । किसी विद्वान गुरु के आश्रम में गुरु सेवा करते हुए अनुशासन पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं । शिक्षा प्राप्ति के पश्चात वैवाहिक बन्धन को स्वीकार करके परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए अर्थोपार्जन द्वारा न केबल पारिवारिक अपितु सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन करते समय हम वैश्य होते हैं । अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करने के पश्चात आत्म केन्द्रित कार्यकलापों से निवृत्त होकर अध्ययन, सेवा एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए हम पुन: ब्राह्मण एवं क्षत्रिय होते हैं । चतुर्थ अवस्था में सब कुछ का परित्याग करते हुए न केवल सांसारिक भोग विलास अपितु परिवार एवं गोत्र का त्याग करने पर पुन: ब्राह्मणत्व एवं शूद्॒त्व को प्राप्त होते हैं | उस अवस्था में जातिवर्ण का विचार त्याग कर शूद्र की भाँति मानव मात्र की सेवा ही हमारा लक्ष्य होता है । त्याग, सादगी, अध्ययन एवं ध्यान हमें ब्रह्मणत्व प्रदान करते हैं । जीवन की परिवर्तित भूमिकाएँ आश्रम धर्म के समानान््तर चलती है । एक हिन्दू के समग्र जीवन के विकास के लिए ये चार आश्रम परस्पर सहयोगी चार सोपान की भाँति है। इस व्यवस्था में क्रमश: आरोहण है, जीवन की सार्थकता है, तथा व्यक्ति की क्षमता एवं अन्त: प्रेरणा के स्वाभाविक विकास का उचित समयपर उचित एवं प्रशस्त मार्ग है । मनुष्य की संवेदनाओं एवं अनुभूतियों के अवरोध का कोई प्रयास नहीं किया गया। व्यक्ति आनन्द, उल्लास, धन धान्य सम्पन्न जीवन जीने के लिये पूर्णत: स्वतंत्र है । लेकिन यह अवश्य . कहा गया है कि किसी वस्तु की अभिलाषा के पूर्व उस वस्तु के संरक्षण की योग्यता प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । इसी उद्देश्य से स्वस्थ शरीर, मन, बुद्धि, प्राण एवं इन्द्रियों की क्षमता को विकसित करने के लिए ही में कठिन अनुशासन में रहते हुए सादगीपूर्ण वातावरण में गहन अध्ययन का प्रावधान किया गया है । भोगवादी अवस्था स्थायी नहीं होती । हिन्दू धर्म में शाश्वत यौवन की लालसा का कोई स्थान नहीं है । मनुष्य की जीवन यात्रा गृहस्थ जीवन के संकीर्ण वृत्त से प्रारम्भ होकर निष्काम सेवा के
द्वारा सामाजिक जीवन के सीमित लक्ष्य को साधती हुई अंत में आत्मानुसंधान के लिए सन्यासाश्रम में परिणति होती है । यही मानव जीवन का अन्तिम एवं चरम लक्ष्य है । प्राचीन ऋषियों की वर्णाश्रम की यही मूल अवधारणा थी न कि आधुनिक विकृत व्यवस्था | आश्रम धर्म आदेशात्मक है न कि विवरणात्मक। दोनों के सादृश्य एवं भिन्नता को समझना नितान्त आवश्यक है ।
३६. वर्णा्रम व्यवस्था के सम्यक् परिपालन की कूंजी क्या है ? इस संकल्पना के आधार हैं यज्ञ एवं संस्कार । पहले हम यज्ञ को ही लें । आजकल यज्ञ का प्रचलित अर्थ है निर्धारित कर्मकाण्ड के अनुसार अग्नि में शाकल्य (घी, काला तिल, जौ, चीनी आदि का मिश्रण) की आहुति देना । लेकिन हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके गूढ़ अर्थ हैं । गीता कहती है –
सहवज्ञा: ग्रजा; उृष्टवा पुरोवाच प्रजापति: /
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्चिष्ट कामुक //
प्रजापति (सृष्टिकर्त्ता) ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा “ इस यज्ञ द्वारा तुम शुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिये इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला “इष्टकामद् होवे ।
अनाद् भवत्ति भ्रृग्रानि पर्ज्यावन्त संभव: /
वज़ादूभवति पर्जन्यो यज़: कर्म समुद्भव: //
समस्त प्राणी अन्न से उत्पन होते हैं, अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य (मेघ, बादल) से । पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है ।
कर्म ब्रह्मोद् भव॑ विद्धि ब्रह्माक्षर सदुद्भवर् ।
,क्स्पात्सव॑ग ब्रह्म तित्यं वज़े प्रतिष्ठितण् //
की उत्पत्ति ब्रह्माजी से होती है और ब्रह्माजी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं । इसलिये सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है । यहाँ दो स्तरों पर कर्म का उल्लेख किया गया है । व्यक्ति गत इकाई के आधार पर तथा जीवन के सम्पूर्ण दृश्य पटल पर निरन्तर करने की प्रक्रिया के रूप में । कर्म जनसामान्य के हित में समर्पण की भावना से किया जाना चाहिये । ऐसा निष्काम समर्पित कर्म ही व्यक्ति तथा सर्मष्टि की रक्षा करने में समर्थ होता है । ऐसा विश्वजनीन विधान ही ब्रह्माण्ड को धारण किये हुए है । अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिये कर्म स्वहितात्म, स्वहित केन्द्रित नहीं होने चाहिये । जब व्यक्ति अध्यात्म में सुस्थापित हो जाता है तब उसके कर्म अहंकार एवं स्वार्थ मूलक कामना से रहित पवित्र एवं बन्धनमुक्त करने वाले हो जाते हैं । गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बेदकालीन प्रचलित और परिचित शब्दों को अभिनव अर्थ में प्रयुक्त किया है । यज्ञ निष्काम एवं जनहित में किए गए कर्मों का सूचक है । बैसे भी अग्नि में आहुति समर्पण के भाव से “इदं न मम” कहते हुए दी जाती है । अत: जीवन के समस्त कार्यों को इसी समर्पण की भावना से करना चाहिये । शुद्ध अन्त:करण से जनकल्याण की भावना से किये गए कर्म व्यष्टि एवं समष्टि सभी का
कल्याण करने बाले होते हैं ।
३७. सदाचारी जीवन जीने की दूसरी कूंजी है संस्कार” इसके लिए मन में संयम एवं उदात्तीकरण की आवश्यकता है । समाजहित को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति विशेष के प्रति किये गए सम्यक् कर्म से चित्त की शुद्धि होकर उपयुक्त समय पर शुद्ध एवं सात्विक संस्कार का निर्माण होता है । बच्चे के जन्म के पश्चात् नामकरण संस्कार, बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है बह अन्नप्राशन संस्कार, विद्या प्रारम्भ के पूर्व विद्याध्ययन संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के पूर्व ‘यज्ञोपवीत संस्कार” (यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्) ही द्विज संज्ञा होती है ।) ब्रह्मचर्य आश्रम की कालावधि में शिष्य गुरु के सान्निध्य में गुरुकुल में रहते हुए अनुशासन पूर्वक अध्ययन का कार्य सम्पन्न करता है । ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् बटुक वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी मानते हुए पवित्र परिणय सूत्र में आबद्ध होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है । गृहास्थाश्रम में जीविफोपार्जन द्वारा अपने परिवार का पोषण करते हुए भी उपासना ध्यान आदि के नित्य नैमित्तिक वेद विहित कर्मों को करते हुए अपने आगामी आध्यात्मिक जीवन के लिये
तत्पर होता है । गृहस्थाश्रमी के लिये स्मृतिकारों की व्यवस्था है कि व्यक्ति को सन्तान कामना, वंश विस्तार की कामना से ही सहवास करना चाहिये। इस प्रकार उसके सुसंस्कृत उदात्त एवं पवित्र जीवन का निर्माण होता है , यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात् मृत देह का अग्नि दाह भी संस्कार की श्रेणी में आता है जिसे दाह संस्कार कहा गया है । दाह संस्कार भी अन्त्येष्टि कहा जाता है जिसका अर्थ है अन्तिम यज्ञ । ये षोडष संस्कार शास्त्र सम्मत है तथा समाज ने विनम्रता पूर्वक इन्हें स्वीकार किया है | अत: व्यक्तित्व निर्माण में इनका असर व्यापक तथा स्थायी रहा । बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी के फलस्वरूप वैदिक ज्ञान की परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी अक्षुण्ण रही। गुरु अपने समर्पित, आज्ञाकारी एबं सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शिष्यों को यह ज्ञान देते थे और इसी प्रकार गुरु शिष्य परम्परा के कारण हजारों वर्षों के कालखण्ड में यह श्रुत ज्ञान अक्षुण्ण रहा । मानव इतिहास में ज्ञान की अखंड परम्परा का अन्यत्र उदाहरण दुर्लभ है । इस आश्चर्य का मूल ‘संस्कारों’ में ही निहित है ।
३८. हिन्दू धर्म में आधार एवं अधिकार के नाम से वर्गीकरण का एक प्रमुख . सिद्धान्त है । सत्ता एवं प्रतिभा के अनुरूप व्यक्ति विशेष के अधिकार एवं स्वत्व निर्धारित होते हैं । हिन्दू धर्म सम्पूर्ण मानव जाति के लिये है, अपरिष्कृत भोगवादी से लेकर परिष्कृत लोकोत्तर वादी (मोक्षकामी) तक के लिये उपादेय । इसीलिए हिन्दू धर्म में सिद्धान्त एवं व्यावहारिक रूप से साधारण कर्मकाण्ड, मूर्ति पूजा, उपासना, आदिम उपासना पद्धति, तांत्रिक उपासना आदि से लेकर निराकार ध्यान उपासना आदि का समावेश है । उदाहरण के तौर पर वैदान्तिक स्तर, सात्विक स्तर, निम्न एवं उच्च कर्मकाण्ड के स्तर तथा स्थूल पूजा के स्तर विद्यमान हैं | अपनी शारीरिक, मानसिक क्षमता, अभिरूचि के अनुरूप साधक उपासना पद्धति का चयन करने में
स्वतन्त्र हैं।
३९. यही है हमारे प्राचीन ऋषियों, मनीषियों, एवं प्रज्ञावान विधिनिर्माताओं द्वारा विकसित हिन्दू धर्म का एक संक्षिप्त परिचय । जीवन को अर्थपूर्ण समग्रता जीनेवाले स्वतन्रचेता व्यक्तियों के जीवन मूल्यों का प्रतिमान इसमें निहित हैं | सुव्यवस्थित सामाजिक परिवेश में सद्भावपूर्ण जीवन जीने की कला है । इसकी संरचना में स्थायित्व के साथ साथ लचीलापन है । इस धर्म में कर्म एवं उपासना के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता है । हिन्दू सनातन धर्म के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करने से पूर्णता, सन्तोष, दिव्यता का अनुभव हो सकता है । व्यक्ति अथवा समाज के भ्रष्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं । व्यक्ति स्वातत्रय के साथ साथ व्यक्तित्व के विकासकी पूरी संभावना इसमें निहित है ।
४०. अब हम हिन्दू-धर्म के सभी सूत्रों को समेटते हुए इसे समग्रता से देखने का प्रयास करें । इस धर्म पर जिस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं उसके विपरीत यह धर्म मतान्धता से मुक्त, अनुभव जन्य, एवं प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप लचीलेपन से युक्त है । इसमें जीवन के समग्र विकास का संपूर्ण सम्यक् रूप से वर्गीकरण किया गया है तथा अपने मनोवेग एवं अन्त:प्रेरणा के विकास का अवसर प्रदान किया गया है । जीवन की चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिये उसको ध्यान में
रखते हुए इसकी संरचना की गई है । यह केवल हिन्दुओं का ही नहीं अपितु समग्र मानवता को श्रेय मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाला धर्म हैं । किसी एक निर्धारित उपासना स्थल, पैगम्बरवाद, पैशाचिकी तथा व्यक्तिगत ईर्ष्यालु देव कल्पना से रहित यह रहस्यवादी आध्यात्मिक सर्वजनीन एवं शाश्वत धर्म है । भावी मानवता के लिये यही एक सर्वाधिक उपयुक्त धर्म है ।
“ये यथा भाम् ग्रप्चन्ते ताम् तथैव भजाम्यहम्’