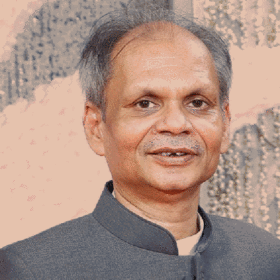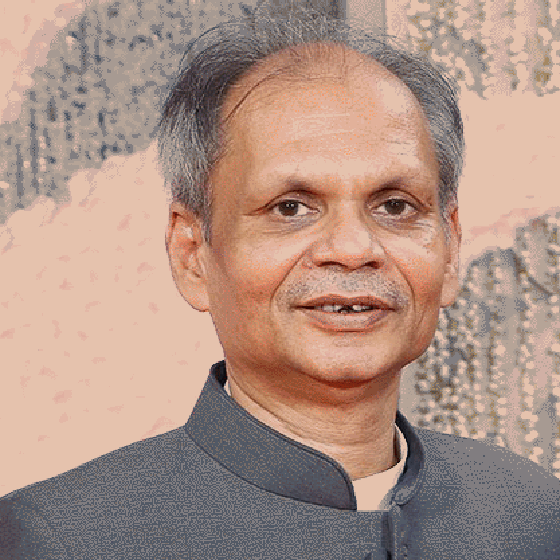An Overview of Vedic Poetry

वैदिक वाद्यमय – एक सिंहावलोकन
by – देवरिशी कलानाथ शास्त्री
बेद भारतीय विद्या की सर्वाधिक मूल्यवान निधि है | विद्वानों का मानना है कि ऋ्म्वेद न केवल भारत का बल्कि समूचे बिश्व हे का प्राचीनतम ग्रन्थ है। भारतीय धर्म और संस्कृति का मूल स्रोत वेद ही है। मनुस्मृति में कहा गया है – बेदोडखिलो धर्ममूलम्। वेद कब लिखे गये इस सम्बन्ध में विश्व के विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इनका समय कुछ विद्वान आज से तीन लाख वर्ष पहले तक ले जाते है जबकि कुछ ईसा से २२०० वर्ष पूर्व तक ले आते हैं। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर जर्मन विद्वान् मैक्समूलर के अनुसार बेद आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व अर्धात् ईसा से लगभग २२ सौ वर्ष पूर्व लिखे गये होंगे। लोकमान्य तिलक ने गाणित ज्योतिष के ग्रमाणों से सिद्ध किया है कि ऋगेद ईसा से ६ हजार वर्ष पूर्व से लेकर ४ हजार वर्ष पूर्व के बीच लिखा गया होगा। वैसे पारम्परिक मान्यता यह है कि वेद अपौरुषेय और अनादि है और जो अलौकिक ईश्वरीय ज्ञान ऋ्षियों ने अपनी अन्तःप्रज्ञा द्वारा जाना उसे ही मंत्ररूप में रख दिया है अत: इनका समय निर्धारित करने जैसी बात अनावश्यक है, वे सृष्टि के ग्राउम्भ में प्रकट हुए थे आदि।
यह उल्लेखनीय है कि हजारों वर्षो से वैदिक मंत्रों का स्वरूप इस देश में उसी प्रकार शुद्ध और अक्षुण्ण बना हुआ है। इसका कारण यही है वैदिक विद्वानों ने वेद पाठ की परम्परा को जीवित रखते हुए अनेक शताब्दियों से ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि एकरु गुरुकुल या गोत्र के लिए कम से कम एक वेद की किसी शाखा को कण्टस्थ करने तथा उसकी परम्परा अक्षुण्ण रखने का दावित्व दिया गया। कुछ वंशों ने दो वेदों का अध्ययन कर द्विवेदी, तीन वेदों का अध्ययन कर त्रिबेदी और चार बेदों का अध्ययन का चतुर्वेदी की उपाधि इसी परम्पय के अनुसार प्राप्त की धी। कहा जाता है कि पहले समस्त वाड्मय एक सम्मिलित ज्ञानराशि के रूप में था जिसका विभिन्न वर्गों और शाखाओं में विभाजन महर्षि वेदव्यास ने किया। उनका नाम भी इसी कारण वेदव्यास पड़ा जिसका अर्थ है वेदों का विभाजन या सम्पादन करने वाला। चार वेद प्रसिद्ध हैं, वेद, सामबेद, यजुर्वेद, अधर्ववेद | यह माना जाता है कि ऋणेद सर्वाधिक प्राचीन है। क्रक् का अर्थ है छन्द या पद्म | इन्हीं उन्दों या पद्यों को गान-बद्ध कर ‘साम’-बेद का उद्भव हुआ जिसका अर्थ है गीत | इसके बाद यजु: अधीत् गद्य में निबद्ध यजुर्वेद बना | कहा जाा है कि सर्वप्रधम ये बेद ही संहिताबद्ध हुए जिन्हें त्रयी कहा जाता धा। ऋगेद में देवताओं की स्तुतियाँ और सृष्टि-विद्ा है, यजुरवेद में यज्ञ का कर्मकाण्ड है और सामवेद में स्तुतिगान। यह त्रयीबेद के नाम से कही जाती थी। बाद में गूढ़ व्यावहारिक क्रियाओं का प्रतिपादन करने हेतु अथर्व क्रषि ने अधर्ववेद रचा किन्तु पाएम्परिक मान्यता यह है कि त्रयी का अर्थ है छन्द, गान और गद्य – ये तीन विधाएँ। चारो वेदों में ये विधाएँ विद्यमान हैं अत: चार्यो को त्रयी कहा जाता है। कोई पूर्ववर्ती या परवर्ती वेद नहीं है। रूपकात्मक ढंग से यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद मूर्ति ॥ अर्थात् पदार्थ हैं (पृथ्वी से सम्बद्ध), यजुर्वेद गति है (अन्तरिक्ष से जुड़ा), सामवेद तेज है (आकाश से जुड़ा) और अधर्ववेद सबका समन्वय है। कहते हैं ग्रन्थ लेखन की परम्परा के अभाव में गुरु वेद मंत्रों को शिष्यों को कण्ठस्थ करा दिया करते थे। इसी श्रवण पम्प से सनातन रूप से चले आने के कारण इन्हें श्रुति कहा जाता था। किन्तु एक मत यह भी है कि श्रुति का तात्पर्य है स्वाजुपूत ज्ञान जो अन्तःप्रज्ञा से स्वतः सुना जाए। उस ज्ञान के आधार पर या स्मरण करके उपजा ज्ञान स्मृति कहा जाता है। इस प्रकांर श्रुति और स्मृति ये शब्द मौलिक ज्ञान और आधारित ज्ञान का भेद बताने के लिए हैं, बाकी लेख की परम्पण तो पहले से ही चल ही रही है। बेदकाल में भी लिपि थी जिसे पथ्यास्वरिल कहा जाता था तथा वर्णमाला थी जिसे ब्रह्मपशि कहा जाता था।
वैदिक वाइमय बड़ा विशाल है। महाभाष्यकार पतंजलि के भाष्य में ऋगवेद की २१ शाखाएँ, यजुर्वेद की १०० शाखाएँ, सामबेद की १००० शाखाएँ तथा अधर्ववेद की ९ शाख्ाएँ धीं इसका उल्लेख मिलता है। लगता है इसमें से अनेक शाखाएँ काल के गाल में समा गई। आजकल ऋग्वेद की शाकल संहिता ही उपलब्ध है। यजुर्वेद के दो भाग हैं – कृष्ण यजुर्वेद जिसमें हन्दोबद्ध ऋचाओं की ग्रधानता है – तथा शुक्ल यजुर्ेद जिसमें गद्य है। कृष्ण यजुव्ेद की तीन संहिताएँ तैतितीय, मैत्रायणी तथा कठ उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काण्व संहिताएँ प्राप्त हैं। सामबेद की कौधुमी, राणायणी, जैमिनीय ३ संहिताएँ उपलब्ध हैं तथा अथर्ववेद की शौनक एवं पैप्पलाद ही प्राप्त हैं | संहिताओं अर्थात् मंत्र समूहों में अब ऋग्वेद में दस हजार चार सौ सड़सठ ऋचाएँ, कृष्ण यजुर्वेद में लगभग साढ़े तीन हजार तथा अधर्ववेद में छ; हजार मंत्र ही आजकल उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार आज वैदिक वाइसय के केवल सत्ताईस हजार तीन सौ सड़सठ पंत्र ही प्राप्त हैं। वेद के इन मंत्रों को हम आज भी उसी रूप में पाते हैं जिस रूप में ये हजारों वर्ष पूर्व ध। यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय और विश्व-सहित्य में अनुपम बात है कि मंत्रों का पाठ माने टेक्स्ट ज्यों का त्यों बना रहे इसमें जरा भी विकृति या परिवर्तन न आ पाये इसके लिए बड़ी विशिष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था हजाएं वर्षों से वैदिक विद्वानों ने कर रखी थी अन्यधा इतनी लम्बी कालावधियों में किसी भी टेक्स्ट में पाठभेद या परिवर्तन आना अपरिडर्य हो जाता है। वेद के टेक्स्ट को बिना मुद्रण की सहायता के भी किस प्रकार अक्षुण्ण और अविकृत रखा जाए इसके लिए प्रत्येक मंत्र के शब्द को सीधा और उल्टा कण्ठस्थ करने तथा एक एक शब्द को आगे पीछे कए-कर के याद करने की ऐसी प्रथाएँ बनाई गई जिससे एक शब्द भी इधर उधर नहीं हो सके। इस प्रकार के अभ्यास्त को आज भी विकृति पाठ कहते हैं। आठ प्रकार के विकृति पाठ प्रसिद्ध हैं। जटा, माला, शिखा, ध्वज, दण्ड, रथ और धन। इस प्रकार वेद के टेक्स्ट को रटने की सहसाच्दियों की परम्परा रही है। ऐसी व्यवस्था के कारण ही वेदों की ऋचाओं में न तो परिवर्त्तन हो पाया, न पाठभेद और न क्षेपक या प्रक्षिप्त अंश ही जुड़ पाए। इसीलिए विश्व के सभी शोध विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि वेद का टेक्स्ट शोध की दृष्टि से अत्यन्त प्रामाणिक और मान्य है।
वैदिक वाइमय का फलक
बेद के मंत्रों का भाष्य तथा उनके दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया इन ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं। इनके भी अनेक प्रकार हैं – ब्राह्मण अर्थात् भाष्य, आरण्यक अथवा दार्शनिक विवेचन, उपनिषद् अथवा बौद्धिक चिन्तन आदि। प्रत्येक बेद के अलग-अलग ब्राह्मण और उपनिषद् हैं। जैसे ऋवेद के ऐतरेय ब्राह्मण, कौड्रीतकि ब्राह्मण और ऐतरेय कौषीतकि आदि आरण्यक तथा उन्हीं नामों की उननिषदें। यजुर्बेद का शतपध ब्राह्मण, तैत्तितीय ब्राह्मण, कठोपनिषद्, बृहदाएण्यक उपनिषद् आदि। सामबेद का ताण्ड्य, षड्विंश आदि ब्राह्मण, छान्दोग्य उपनिषद् केनोपनिषद् आदि और अधर्ववेद का गोषथ ब्राह्मण मुण्डकोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद् आदि। सनातनधर्म की परम्परा की मान्यता यह है कि संहिता और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि सभी मिलकर वेदसाहित्य कहलाते हैं। काल की गति से वेदों के मंत्रों के अभ्यास में धीरे धीरे हास होता गया और उपनिषदों आदि का अभ्यास करते करते विद्वानों ने कई उपनिषदें और जोड़ दीं – भक्तिआन्दोलन के साथ भक्तिमार्ग की उपनिषदें भी जुड़ती गई। उन्नीसवीं सदी के अन्त में महर्षि दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदमंत्रों के अभ्यास के उद्देश्य से नये पुनरुद्धार आन्दोलन को बल दिया। इस आर्य समाज को केवल वेदों की संहिताएँ ही प्रमाण रूप से मान्य हैं, अन्य ग्रन्थ नहीं। वेदों के अनेक भाष्य लिखे गये – जिनमें आचार्य सायण का भाष्य प्रमुख है। वैसे दुर्ग, उत्बट, महीघर आदि अनेक भाष्यकार हुए हैं।
वैदिक कर्मकाण्ड और आचार संहिता के प्रतिपादन के लिए श्रौतसूत्र, स्मार्तसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्मसूत्र आदि तथा शिल्पशास्र के विवेचन के लिए शुल्वसूत्र लिखे गये हैं इन्हें कल्प कहा जाता है। बैदिक व्याकएण सिखाने के लिए प्रातिशाख्य, उच्चारण सिखाने के लिए शिक्षा, छन्दः शाख्र सिखाने के लिए छन्द, शब्द शास्त्र सिखाने के लिए निरूक्त, लिखे गये। इन्हें वेदांग कहा जाता है। इस प्रकार अपरिमित ग्रन्थ राशि वेदों पर आधारित आज भी उपलब्ध होती है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, नाट्य आदि उपवेद तथा शिक्षा, कल्प निरक्त, व्याकरण छन्द और ज्योतिष वेदांग कहे जाते हैं।
बेदों में सभी प्रकार की ज्ञानराशि निहित है। अग्नि, वायु, सूर्य आदि प्राकृतिक महाशक्तियों की स्तुतियाँ, सृष्टिविद्या, ज्योतिष, शरीए-शाख््र, सामाजिक कल्याण के अतुष्ठानों के सिद्धान्त, दार्शनिक चिन्तन आदि सब प्रकार का साहित्य वेदों में उपलब्ध है। प्रत्येक मंत्र जिस विशेष देवता को लक्ष्य करके लिखा गया है उसका उल्लेख, जिस ऋ्रषि के मानस में उसका आविर्भाव हुआ उसका उल्लेख, जिस छन्द में लिखा गया उसका उल्लेख, इस प्रकार का सम्पादन करके वेदव्यास ने बेदों को पृथक भागों में विभाजित किया था, ऐस्ता माना जाता है। इसके अनुसार ऋणेद १० भागों में विभाजित है जिन्हें मण्डल कहा जाता है। प्रत्येक मण्डल में अनेक सुूक्त हैं। जिनमें अनेक मंत्र हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामबेद और अधर्ववेद भी मण्डलों और सूक्तों में विभाजित हैं।
जैसा ऊपर बताया गया है वेद संहिताओं में से बहुत सी अनुपलब्ध हैं। जो उपलब्ध हैं उनमें से प्राय: सभी मुद्रित और प्रकाशित हो चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बोडेन चेयर के प्रोफेसर फे० मैक्समूलर ने सर्वप्रधम १८४८ ईस्वी में ऋगेद का मुद्रण करवाया था जो १८७५ तक होता रहा। तभी से विश्व में वाइमय की धूम मच गई। एच०.एच०. बिल्सन, ग्रिफिथ और स्टीबेन्सन ने अंग्रेज़ी में रॉध के शिष्य गोल्डनर ने तथा बार्नूफ आदि विद्वानों ने जर्मन में वेदों के अनुबाद किए। कीथ, एगलिंग आदि ने अन्य बैदिक वाड्मय के अनुवाद किए । जर्मनी, इंगलैण्ड, अमरीका आदि में वैदिक वाइमय का अनुशीलन होने लगा। भारतीय भाषाओं में भी बैदिक वाइमय के विशाल फलक पर अनुवाद उपलब्ध हैं। इस प्रकार वेद चाड्मय अत्यन्त विशाल है और उस पर लिखा गया साहित्य तो अपरिमेय ही है। यहाँ वेद संहिताओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।
ऋग्वेद : संहिता और शाखाएँ
यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ऋग्वेद मानव के पुस्तकालय की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। आज इसकी जो संहिता मुद्रित रूप में उपलब्ध है वह मैक्समूलर द्वारा सर्वप्रधम इंग्लैण्ड में देवनागरी टाइप में १८४८ ई० में मुद्रित कराई गई थी। वैसे पतंजलि ने महाभाष्य में पस्पशाहिक में लिखा था एकर्विशतिघा बाहवृच्यम् जिसका तात्पर्य यह माना जाता है कि इसकी २१ शाखाएँ थीं जिन्हें कुछ २१ संहिताएँ भी मानते हैं किन्तु आज जो विशाल संहिता मिलती है वह शाकल संहिता कहलाती है जो विदग्ध कल्य द्वारा संकलित होने के काएण शाकल कहलाती है। जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार शाकलनगरी (पंजाब के उत्तर में मद्रदेश की राजधानी) का विद्वान् महर्षि शाकल्य कहलाया जिसका असली नाम देवमित्र धा। उसने ऋग्वेद का संहिताकरण किया था।
ऋगेद संहिता दो तरह से विभाजित हैं मण्डलों मे और अष्टकों में | इसके दस मण्डल हैं और १०२८ सूक्त हैं। ८५ अनुवाक हैं २००८ वर्ग हैं। अष्टकों के वर्गीकरण के अनुसार ८ अष्टक, ६४ अध्याय और २००८ वर्ण हैं। प्रथम मण्डल में १९१, ट्वितीय में ४३, तृतीय में ६२, चतुर्थ में ५८, पंचम में ८७, षष्ठ में ७५, सप्तम में १०४, अष्टम में ११४, नवम में १०३ और दशम मण्डल में १९१ सूक्त हैं। प्रथम और दशम मण्डलों में अपेक्षाकृत परवर्ती ऋचाएँ भी समाविष्ट हैं जबकि दूसरे से लेकर आठवें तक प्राचीनतम ऋचाएँ हैं ऐसा पाश्चात्य शोध विद्वान् मानते हैं। प्राचीन आचार्यों ने वेदों का एक एक अक्षर गिन कर अभिलिखित कर दिया था। झौनक की अमुक्रमणिका में सूचना है कि ऋग्वेद संहिता में १०५८० मंत्र १५३८२६ शब्द और ४३२००० अक्षर हैं। इन अक्षरों से मन्वन्तरों की गणना निकल आती है।
वैसे ऋग्वेद की शाखाओं में शाकल, बाप्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडूकेय ये पाँच गिनाई जाती हैं। पं. भगवद्दत्तजी ने वैदिक बाडमय के इतिहास में २७ शाखाएँ यिनाई हैं जिनमें मुदुगल, गालव, शालीय, वात्स्य, रौशिरि, बाध्य, अग्रिमाठर, पताशर, जातूकर्ण्य, आश्वलायन, शांखायन, कौशतकी, महाकौषीतकी, शांब्य, मांडूकेय, बहबूच, फैंय, उद्दालक, ‘शतबलाक्ष, गजबाष्कलि, भरद्वाज, ऐतरेय, वशिष्ट, सुलभ और श्येनक शामिल हैं। आज भी शाकल, आश्वलायन और शांखावन शाखाध्यायी विद्वान् भारत में फैले हुए हैं।
प्रत्येक बेद की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ लिखे गये जिनमें वेदमंत्रों के यज्ञादि में प्रयोग की विधि भी बताई गई। उनमें निहित ज्ञान का विवेचन आरण्यकों में किया गया और उनमें निहित दार्शनिक चिन्तन का व्याख्यान उपनिषदों में किया गया। इस प्रकार संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् मिलकर बेद वाइमय का मूल पाठ या टेक्स्ट कहा जा सकता है।
ऋग्वेद का कलेवर जितना विशाल है उतना ही विशाल है उसकी विषय सामग्री का फलक | इसमें विभिन्न ज्ञानशाखाओं से सम्बद्ध सूक्त हैं जो दस मण्डलों में विभाजित हैं। विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रणीत (दूसरे शब्दों में ‘दृषट’) ये सूक्त कभी विभिन्न देवताओं को सम्बोधित कर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की कामना करते हैं कभी ऐहलौकिक अभ्युदय का आशीर्वाद देते हैं, कभी ज्ञान विज्ञान की जानकारी देते हैं। विभिन्न छन््दों में निबद्ध सूक्त (जिनमें अधिकतर एक सूक्त में त्रिष्टू, अनुष्ठप या गायत्री जैसे किसी एक छन्द के ही मंत्र अर्थात् ऋचाएँ निबद्ध हैं) अपनी गरिमामय शैली में जिस ज्ञान सामग्री का रहस्य बतलाते हैं उसमें सृष्टिविज्ञान, प्राणविद्या, सोमविद्या, मधुविद्या, अनुशासन, जीवनविज्ञान आदि अनेक विषय हैं। कुछ तो रूपात्मक शैली में ऐसे रहस्यमय ढंग से सृष्टि का विज्ञान बतलाते हैं कि उनको ‘डिकोड’ कस्के ही उनका अन्तर्निहित रहस्य जाना जा सकता है।
इस प्रकार के विज्ञान रहस्यों को समाहित करने वाले प्रमुखत: दो मण्डल हैं – प्रथम और दशम जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वे सूक्त भी शामिल हैं जिन्हें भाववृत्त सूक्त अर्थात् सृष्टि के इतिहास के सूक्त भी कहा जाता है जिनमें बतलाया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, कैसे सारी सृष्टि उद्भूत हुई, कैसे पृथ्वी, आकाश, ग्रह आदि पैदा हुए। इनके प्रधम अक्षरों के आधार पर इनके नाम विद्वत्समाज में प्रसिद्ध हो गए हैं जैसे नासदीय सूक्त (१/१२९), अस्यवामीय सूक्त (१/१६४), पुरुष सूक्त आदि। पृथ्वी पर जीव के उद्धव और प्राणियों तथा मानवों के उदविकास का वर्णन जिन ऋ्रचाओं में है उन्हें पुरुष सूक्त कहा जाता है। ऐसे पुरुष सूक्त ऋग्वेद मे भी हैं, यजु्ेंद में भी, अन्यत्र भी।
वैदिक संस्कृति यज्ञ संस्कृति कही जाती है। यज्ञ का अर्थ है किसी देवता के उद्देश्य से द्रव्य का विसर्जन अर्थात् अंग्रि में हे का होम किन्तु उसका उद्देश्य होता है दो पृथक् द्रव्य के संभिश्रण से किसी तौसरे पदार्थ का उद्भव । बड़ एक सामूहिक, हपग्रद, ज्ञानार्नन हेतु किया जाने वाला सुनियोजित सत्र होता था जिसके अनेक प्रकार और प्रयोग वेदों में बतलाए गए हैं। किस प्रकार यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, किन देवताओं ने प्रसन्न होकर इस देश को क्या अबदान दिया इसका संकेत भी वेदों में मिलता है। चेद के प्रमुख देवता हैं इन्द्र, वरुण, पूषा, अर्यमा, सूर्य, रुद्र, चौ, वसु, आदित्य, अश्विनीकुमाए आदि।
इस धरती के बहुमूल्य पदार्थों का, जन्म मृत्यु के रहस्य का, ब्रह्माण्ड के पिण्डों का, आत्मा का तथा अल सभी प्रकार के झतव्य पदार्थों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलना इसी तथ्य को पुष्ट करता है कि बेद हमारी समग्र ज्ञाननिधि के संकलन के रूप में सुरक्षित है। उनकी बहुत सी सामग्री आज अतुपलब्ध है, जो उपलब्ध है वह भी विविध ृष्टियों से सम्पादित और वर्गीकृत है! उससे अनुमान ही कर सकते हैं कि हमारी ह्ानसम्पदा की पहम्परा कैसी थी।
यजुर्वेद
यजुर्वेद के दो भाग है कृष्ण यजुवेंद और शुक्ल यजुवेंद। यजु का शब्दार्थ है यज्ञ यजुर्वेद में है यह माना जाता है। शुद्ध गद में जो भाग है उसे शुक्ल तथा जिसमें छन्द भी मिले हुए है, ब्रह्म भी अर्थात् याध्ाएँ भी उसे कृष्ण कहा जाता है अर्थात् प्य और गद्य मिले जुले। जुवेंद मूलतः यद्ञ के कर्मकाष्ड का चेद है जिसमें विविध बच्चों का विधान है, देवस्तुतियाँ हैं, साध में गाणित, विज्ञान, शुभकामनाएँ, स्वस्तिवाचन, शब्दकोश, समाज के विविध कार्यकलापों के शास्त्र आदि भी शामिल हैं। यजुर्वेद की सौ शाखाएँ कमी रही हॉंगी ऐसा माना जाता है क्योंकि प॑जलि ने लिखा है” एकशतमध्वरयुशाखा: किन्तु आजकल कृष्ण की तीन और शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ मिलती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैतिरीय, मैत्रायणी और कठ शाखाएँ तथा शुक्ल बजुर्वेद की काष्व, और बाजसनेय, वाजसतेय में माध्यंदिन भी समाविषट है। वैसे काप्व, आध्यंदिन, जाबाल, बुधेय, शाकेय, तापनीय, काणीस, पौड़ंवहा, आवर्तिक, परमाद्रतिक, पाराशरीय, बैनेय, बौधेय, यौधेय और गालव इन सभी १५ शाखाओं को वाजसनेय संहिता में समाविष्ट माना जाता है। चरणव्यूह के उल्लेखातुसार इनमें १९०० मंत्र हैं।
कृष्ण यजुवेंदे मंत्र संख्या १८००० बताई जाती है। इसमें सात काण्ड है। धत्येक काण्ड अपाठकों और अलुवाकों में विभक्त है। शुक्ल यजुर्वेद के ४० अध्याय हैं जिनमें से अन्तिम अध्याय इशावास्यमिद सर्व मंत्र से शुरू होता है और हिरण्मयेन पात्रेण से समाप्त होता है। इसे ही ईशावास्थ उपनिषद् कहा जाता है क्योंकि इसमें रहस्यवाद भी है, दर्शन भी, पराविद्या भी है और परमतत्व की जिज्ञासा और विवेचन भी । यह वेद का अन्तिम अध्याय होने के कारण उपनिषदों के दर्शन को बेदान्त कहा जाने लगा। यजुर्वेद में रुद्र देवता को सम्बोधित जो मंत्र हैं उनके आठ अध्यायों को कद्राषटाध्यायी कहा जाता है जो शैव सम्प्रदायों के मूल प्रेरक माने जाते हैं। इनमें गणित का, समाज के विभिन्न कार्यकलापों का, आजीविकाओं, वर्गों आदि का ज्ञान निहित है। उत्तर भारत में शुक्लयजुर्वेद का और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद का विशेष कर तैत्तितीय शाखा का अधिक प्रचार है।
प्रत्येक बेद के उच्चारण की शैली अलग-अलग निर्धारित है। ऋग्वेद के अनेक मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में भी समाहित हैं। अतः कृष्ण यजुर्वेद और ऋग्वेद की ‘पाठशैली में कुछ समानता है, शुक्ल यजुर्वेद की पाठशैली पृथक् है जिसमें स्वर की पहचान कराने हेतु हाथों का और उँगलियों का परिचालन भी सिखाया जाता है।
यजुर्वेद के चालीस अध्यायों में विभिन्न ज्ञान शाखाओं की सामग्री संगृहीत है जिसका फलक भी इसी प्रकार व्यापक है जिस प्रकार अन्य वेदों का। चैसे यह माना जाता है कि यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ की विधियों के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संकलित किया गया, यह भी माना जाता है कि ऋग्वेद पद्यबद्ध और अजुर्ेद गद्यबद्ध है किन्तु यजुरेद में उन्द भी मिलते है, यज्ञ के अतिरिक्त कार्यो की ज्ञान सामग्री भी । एक कथा के अतुसार याइवलक्य ने सारा चेद कंठस्थ कर लिया धा, वैशंपायन के आदेश पर उन्होंने उसे उगला तो उसमें से कुछ ऋचाएँ तित्तिरि (तीतर) बनकर ऋषियों ने चुन लीं, वह कृष्ण यजुर्वेद (तैतिरीय शाखा) हो गया। आज कृष्ण यजुर्वेद में ऋचाएँ (उन्दोबद्ध) भी मिलती हैं, गद्य भी और उनकी व्याख्या भी (जिसे ब्राह्मण कहा गया है) । इस मिले जुले स्वरूप में यज्ञ के मंत्र और विधियाँ ही हैं। वैसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिन शाखा) दोनों में यज्ञ के लिए प्रयुक्त मंत्रों के अलावा सृष्टि विद्या भी है, गणित के पहाड़े भी, इन्द्र, विष्णु आदि के सूक्त भी, पुरुष सूक्त भी।
वेदकाल का प्रमुख देवता था सूर्य जो समस्त सृष्टि का नियामक माना गया। इसकी स्तुति के मंत्र सभी वेदों में मिलते हैं।गायत्री मंत्र भी सूर्य की स्तुति का मंत्र ही है। वैसे महर्षि दयानन्द आदि जिन विद्वानों ने वेद में एकेश्वस्वाद का प्रतिपादन बतलाकर उसकी व्याख्या की धी, उन्होंने गायत्री मंत्र को परमपिता परमेश्वर की स्तुति के रूप में व्याख्यात किया है।
यजुवेंद में आठ अध्याय जो रुद्र देवता को समर्पित हैं रुद्राष्टाध्यायी कहे जाते हैं। उनमें रुद्र देबता के अतिरिक्त अन्य देवताओं की स्तुतियाँ भी हैं, भारद की विभिन्न विद्याओं के, पेशेवर वैज्ञानिकों और उनके पेशों के ठघा गणित की सारणियों के विवरण भी हैं। इनका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि रुद्राष्टाध्यायी को कठंस्थ करने के बहाने हमारे बुुद्धिजीवी विभिन्न विद्याओं का ज्ञान भी हस्तगत करलें।
शुक्ल यजुवेंद में निहित ज्ञान-विज्ञान की तथा य्ञ प्रक्रियाओं की व्याख्या करने हेतु लिखा गया ग्रन्ध शतपध ब्राह्मण कहलाता है जिसमें वैदिक संज्ञाओं, बचनों और संकेतों में निहित ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टि और तर्कपूर्ण अभिगम से विवेचन किया गया है। कहा जाता है कि इसका प्रवर्तन याज्ञवल्क्य ने किया था | इसी ब्राह्मण के आधार पर अनेक विद्वान् बेद में निहित विज्ञान का प्रतिपादन करते रहे हैं जिनमें जयपुर के पं० मधुसूदन ओझा विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वेदों में निहित सृष्टि विज्ञान, प्राणविद्या, आदि का प्रतिपादन अपने २०० से अधिक विशाल ग्रन््धों में किया है। उनकी मान्यता है कि वेदों में तत्कालीन भारत का इतिहास भी है जबकि आर्यस्रमाज की यह मान्यता है कि बेदों में इतिहास नहीं है, वे तो उससे पूर्व के हैं।
ब्राह्मण एवं आरण्यक
यह सूचित किया ही जा चुका है कि जिस प्रकार ऋखेद के साथ दो ब्राह्मण ग्रन्थ जुड़े हुए हैं (एतरेय ब्राह्मण और कौपीतकि
ड्राह्मण) उसी प्रकार यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण और तैत्तितीय ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के साथ जैसे ऐतरेय
आएण्यक और कौपीतकि आएण्यक तथा एतरेयोपनिषद् और कौपीतकि उपनिषद् जुड़ी हुई है, वैसे यजुर्वेद के साथ कठोपनिषद् तथा बृहदारण्यक उपनिषद् जुड़ी हुई हैं। संहिताओं में मंत्र (पद्च और गद्य दोनों में निबद्ध) जिस ज्ञान का संकेत देते हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ उसका विज्ञान बतलाते हुए भाष्य प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक चिन्तन और परमदत्त्व की जिज्ञासा शान्त करले हेतु दर्शन का प्रतिपादन उपनिषदों का कार्यक्षेत्र है।
सामवेद
सामवेद बेदत्रयी का अभिन्न अंग है। ऋग् यजु: और साम ये तीन वेदत्रयी कहे गये हैं। इसीलिए क्रूग् यजु:ः साम और अथर्व इन चार वेदों में अधर्ववेद परवर्ती है ऐसा कुछ विद्वान् मानते थे किन्तु वेदों में पद्य गद्य और गीति इन तीन शैलियों को त्रयी कहा जाता है इसलिए चारों बेद ही त्रयी हैं और सभी समान रूप से एक ही वेद स्वरूप के अंग हैं, यह सप्ट उर7 “मे विद्वानों ने चारों को समान रूप से पुरातन माना है। दोनों ही दृष्टियों से सामवेद काफी पुरातन सिद्ध होता है। स्वयं ऋेद थे रूम द७ साम का उद्ठेख हुआ है
उप नो देवा अबसा गमन्तु अंगिरसा सामधिः स्तूयमाना:।
इन्द्र इन्द्रियर्मरूतो मरुद्धिरादित्यैनों अदिति: शर्म यसत्।
उद्ातेव शकुने साम गायसि।.
इत्यादि ऋ्चाओं में स्तुति या स्तोत्र के आर्ध में सामगान का उद्ठेख आवा है। साम का अर्थ सुखकर भी किया गया है, स्यति नाशयति विघ्नात् कह कर विध्ननाशक और समयति संत्तोषयति देवान् कहकर देवों का संतोषक भी इसे बताया गया है। अम से सहित साम व्युत्पत्ति करके बाक् ही साम है यह भी कहा गया है। एतदुह बाव साम यद् वाक्। (जे० उ० ब्रा०२/१५/४) सामवेद में गीतियाँ हैं और उदगीध में उद्गाता इनका गान करता है इसीलिए यह गेयबेद है, संगीत की आदिम अभिव्यक्ति है,यह माना जाता है। छात्दोग्य उपनिषद् कहती है कि घोर आंगरिस ने देवकी पुत्र कृष्ण को दर्शनदीक्षा देते समय साम के गानतत्व का मर्म भी समझाया धा। तब छालिक्य नामक नई गानशैली का उद्भव हुआ प्राचीनतम वाद्ययनतरों, दुन्दुभि, वेणु और वीणा पर अनेक राग-रागिनियों का अवतरण हुआ।
सामवेद के लिए सहख्वर्त्मा सामवेद: कहा जाता है जिसका कुछ लोग यह अर्थ लगाते हैं कि इसकी एक हजार शाखाएँ्थीं। कुछ का कहना है कि हजारों गानशैलियों के अर्थ में ही यह शब्द आया है। आज तो केवल तीन शाखाएँ ही सामवेद की पिलती हैं – कौधुम संहिता, जैमिनीय संहिता और राणायणीय संहिता। कौधुम का गुजरात में, जैमिनीय का कर्णाटक में और ‘राणावणीय का महाराष्ट्र में विशेष प्रचार है। पं० भगवददत्त जी ने अपने वैदिक वाढमय के इतिहास में यह उल्लेख भी किया है कि महाभासत के १५० वर्ष पूर्व हुए उपन््यु ने एक औपमन्यव शाखा और चलाई थी किन्तु यह आज नहीं मिलती | सामवेद में कुल १८७५ मंत्र मिलते हैं जो ग्राव: सभी ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। केवल ७: मंत्र ऐसे हैं जो केवल सामवेद में हैं अन्यत्र नहीं। इन ऋचाओं को गानशैली, स्वरवितान और समयविस्तार से ही साम का रूप मिलता है। यह माना जाता है कि क्रचा का पाठ जितने समय में होता है उससे तिगुने समय में साम गाया जाता है। इसीलिए त्रक्रच॑ साम कहा गया है। ऋच्चध्यूर्षु साम गीयते कहकर तथा छात्दोग्योपनिषद् ने या क्रक् तत् साम कहकर ऋग्वेद और सामबेद का जो अविनाभाव सम्बन्ध सूचित किया है वह प्रत्यक्ष भी दिखलाई देता है।
ऋ्रक्साम के इस सम्बन्ध को विज्ञानवादियों ने बड़े अनूठे प्रतीकात्मक ढंग से समझाया है। मधुसूदन ओझा ने स्पष्ट किया है कि बेदतत्व को समझाने के लिए यदि एक पिण्ड की कल्पना की जाए तो ऋक् उसका व्यास है और साम उसकी परिधि है। वैसे भी व्यास से परिधि लगभग तीन गुनी होती है। इसीलिए विष्कंभ को ऋक् और परिणाह को साम कहा गया। किसी भी बस्तुपिण्ड के साक्षात्कार होते ही हमें उसका परिणाह या परिधि ही दिखाई देती है इसीलिए सामबेद को विभूतिबेद या वितानवेद भी कहा जाता है। अध्यात्म का अधिदेव के साथ स्वरवितान के द्वारा तारतम्य स्थापित करना ही इसका कार्य है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ” ने कहा है वेदानां सामवेदोस्मि। तत्वविज्ञान की दृष्टि से ऋछ् को अग्नि का बज्चु को वायु का साम को आदित्य का और अथर्व को आप; का रूप बताया गया है।
सामवेद की अधिकांश कचाएँ गायत्री और जगती हों में हैं। दोनों गेय हैं। दोनों का अर्थ और ब्युत्पति भी यही है कि जो गाई जा सकें। इसीलिए विशिष्ट स्वरवितान और प्रस्तार के साध आज भी वैदिक इनका सस्वर गान करते हैं। गायक जिस प्रकार आलाप में ‘आ’ आदि का उच्चारण करता है उसी प्रकार साम का उद्गाता भी उ, ह, वा आदि शब्दों का उच्चारण करता है। लगता है सोमसस बनाते समय या अन्य हर्ष के अवसरों पर देवों को प्रसन्न करने के लिए आनन्दमग्र होकर आर्य लोग सामगान द्वारा सामूहिक संगीत की अवतारणा करते होंगे।
इस गानशैली की अनेक प्रणालियाँ उद्विकसित हुई। छान्दोग्य में हिंकार, प्रस्ताव, उदगीथ प्रतिहार और निधान इन पाँच अंगों का उद्देख मिलता है। ब्राह्मण ग्र्थों में उद्गीत, अनुगीत और आगीत का उद्ेख मिलता है। कु, ग्रधमा, द्वितिया, चतुर्थी, मंद, अतिस्वार्य आदि लयों के नाम भी पाये जाते हैं। इन्हीं से रागतगिनियों का उद्भव और संगीतशास्तर की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है
सामबेद की ऋक् और यजु याने पद्य और गद्य दोनों गेय हैं। ऋचा समूह को आर्चिक और यजु: समूह को स्तोक कहते हैं। इस बेद की शाखा के दो भाग हैं – पूर्वार्चिक और उत्तराचिंक। पहले भाग में ग्राम्यगीत और आएण्यगीत तथा दूसरे भाग में ‘ऊहगीत और ऊद्यगीत संकलित हैं। महर्षि जैमिनि को सामबेद का प्रथम द्रष्ट माना जाता है। उन्होंने इसकी दीक्षा अपने पुत्र या शिष्यसुमन्तु को दी, सुमन्तु ने सृत्वा को, सृत्वा ने सुकर्मा को, सुकर्मा ने सूर्यवर्चासहस्ल को | फिर इन्द्र ने पौष्यंजी को । इसके बाद हिएण्यनाभ, प्राच्यसामग, लौगाक्षि, कुथुमी, कुशीति और लांगली आदि की परम्परा पाई जाती है। लौगाक्षि की शिष्य परम्परा में वाण्ड्यपुत्र राणायण, सुविद्वान् मूलचारी, साकेति पुत्र और सहसात्यपुत्र आदि हुए।
सामवेद की कौधुमीय संहिता के ब्राह्मणग्रन्थ चालीस अध्यायों में विभक्त हैं। इनमें पाँच ब्राह्मण संमाविष्ट हैं – ताण्ड्य ब्राह्मण जिसे पंचविशन्राह्मण भी कहा जाता. है, षड्विंश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, और छान्दोग्य ब्राह्मण! यही छान््दोग्य उपनिषद् है। जैमिनीय संहिता के ब्राह्मण ग्रन्ध हैं जैमिनीय ब्राह्मण और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण। इन्हें ही आर्षेय ब्राह्मण और छात्दोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। तलबकार अर्थात् केनोपनिषद् इसी से सम्बद्ध मानी जाती है। जैमिनीय शाखाध्यायी कर्णाटक में आज भी हैं। इस शाखा के ग्रन्थ कुछ समय पूर्व ही उपलब्ध हुए हैं। एक यूरोपीय विद्वान् डॉ० कैलेंड ने जैमिनीय संहिता का सम्पादन और प्रकाशन किया धा। जैमिनीय श्रोतसूत्र और गृह्यसूत्र भी उपलब्ध हैं।
कौधुम शाखा के कल्पसूत्र का नाम मशककल्पसूत्र और श्रोतसूत्र का नाम लाटचयायन श्रोतसूत्र है। गोभिलगृह्यसूत्र इसी शाखा का है। राणायणीय शाखा कौधुम संहिता के ब्राह्मणों तथा उपनिषद् का अनुसरण करती है। इनका श्रौतसूत्र और गृह्ममूत्र ही अलग मिलता है। इनका श्रौतसूत्र है द्राह्यायण श्रौतसूत्र और गृह्मसूत्र है खादिर्गृह्मसूत्र ।
आज कुछ सामबेदी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक और काशी में सामोच्चारण की परम्पए को जीवित रखे हुए हैं किन्तु काल की गति के साथ यह परम्परा बड़ी तेजी से लुप्त होती जा रही है।
यह सूचित किया ही जा चुका है कि सामवेद का ब्राह्मणग्रन्ध है ताण्ड ब्राह्मण । षड्विंश ब्राह्मण भी सामवेद से जुड़ा हुआ है। छान्दोग्य उपनिषद् तथा केनोपनिषद् सामबेद की उपनिषदें हैं; ठीक उसी प्रकार जैसे अधर्ववेद के साथ गोपथब्राह्मण जुड़ा हुआ हैतथधा मुण्डकोपनिषद् एवं प्रश्बोपनिषद् अधर्ववेद की उपनिषदें मानी जाती हैं।
अथर्ववेदः
भास्तीय संस्कृति के मूल आधार ४ वेद विश्व में प्रसिद्ध हैं – ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधर्ववेद। इन चारों वेदों को प्राचीन परम्परा में अपौर्षेय और अनादि वाणी माना जाता है। वैसे भी ये विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इन चारों वेदों की प्राचीनता वैसे तो असन्दिष्य है किन्तु कुछ शोध विद्वानों का यह मत है कि चौधा बेद अथर्ववेद बाद में जुड़ा। मूलत: तीन बेद ही धे जिन्हें त्रयी कहा गया। गीता में, मनुस्मृति में और अन्य स्थानों पर जो ‘बेदत्रयी’ शब्द है उसे देखकर ही ऐसे विद्वान् यह कहते हैं किन्तु अब अनेक प्राचीन ग्रन्थों के साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट कर दिया गया है कि चारों वेद प्राचीन हैं, अधर्ववेद बाद में जुड़ा हुआ हो सो बात नहीं है। त्रयी कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में तीन विधाओं में मंत्र और वाक्य मिलते हैं, पद्म में, गद्य में और गीतियों में । इन्हें ही त्रयी कहां गया है और इसका अर्थ यह नहीं है कि बेद केवल तीन ही हैं। ऋग्वेद में पद्य ही अधिक हैं, सामवेद में गीतियाँ और यजु्वेद में गद्य। अधर्ववेद में पद्य भी हैं और गद्य भी। यह माना जाता है कि प्राचीन आर्यों का सम्पूर्ण ज्ञान जिसे वेद कहा गया है, पहले एक साथ विशाल वाइमय के रूप में था, उसे सम्पादित और वर्गीकृत करके चार वेदों में बाँठा गया। तैत्तितीय संहिता और पुराणों में बताया गया है कि सुविधा के लिए विशाल बेद को चार भागों में बाँटा गया। ऐसे सम्पादन २८ बार हुए। इन सम्पादकों को बेदव्यास कहा गया।
इस प्रकार सम्पादित चार वेदों में अथर्ववेद को चौथा और अन्तिम माना जाता है। शायद इसी कारण कुछ पाश्चात्य विद्वानों नें इसे बाद में मान लिया और यह कहा कि यह शतपथ ब्राह्मण के भी बाद की रचना है क्योंकि इसमें तंत्र और मंत्र-विद्या वर्णित है और अधर्वबेद शब्द ईरान के अधर्वन शब्द से निकला है। यह बात तो सच है कि अधर्ववेद में मंत्र-विद्या, तंत्र के अनेक प्रयोग, टोने-टोटके, दबाओं के प्रयोग आदि वर्णित हैं किन्तु बह बाद में बना, यह धारणा विद्वानों को मान्य नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत की बहुत सी विद्याएँ अरब देशों में अनुबादों के जरिवे बहुत पहले से जाती रही हैं। जिन महत्वपूर्ण ग्रग्थों का फास्सी में अनुवाद हुआ उनमें अधर्ववेद प्रमुख है। ‘आइने अकबरी’ में संकेत है कि यह फारसी अनुवाद अकबर के पुस्तकालय में सुरक्षित धा। जिस प्रकार ऋणद में प्राकृतिक शक्तियों, तत्वों और देवताओं के यूक्त प्रमुख हैं, यजुर्वेद में कर्मकाण्ड और सामवेद में स्तुतियाँ, उसी प्रकार अधर्ववेद में इहलोक के व्यावहारिक प्रयोग की, मानव जीवन के उपयोग की अनेक विद्याएँ वर्णित हैं.जो मानव के दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक मानी जाती थीं। दूसरे शब्दों में इसे तकनीकी ज्ञान भी कहा जा सकता है इस दृष्टि से अधर्ववेद का अनूठा ही महत्व है।
यह माना जाता है कि अधर्वा नामक क्रषि ने इन विद्याओं का साक्षात्कार किया इसलिए इसका नाम अधर्ववेद पड़ा । वस्तुत: अधर्वा ऋषि और आंगिसस क्रषियों ने जो विद्याएँ बताईं उनका अभिलेख है अधर्ववेद इसीलिए इसे अधर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। जितने मंत्रों में तंत्र विद्या, टोने-टोटके और औषधियाँ बतलाई गई हैं वे अधर्वा ने बताई हैं और मारण, उच्चाटन आदि की विद्याएँ आंगिरसों ने बताई हैं ऐसी मान्यता है। वैसे अधर्ववेद में इन विद्याओं के अतिपिक्त दार्शनिक विवेचन भी है, ब्रह्मविद्या भी है, आशीर्वाद भी है, प्रार्थनाएँ भी, और स्तुतियाँ भी। यह बेद २० काण्डों में विभक्त है। ये २० काण्ड ४८ प्रपाठकों में विभाजित हैं। अधर्ववेद में ७६० सूक्त हैं और लगभग ६००० मंत्र हैं। प्रसंगवश स्थान-स्थान पर ऋग्वेद की ऋचाएँ भी ले ली गई हैं जिनकी संख्या लगभग १२०० है। चूंकि लौकिक विद्याओं के विवेचन में श्राद्ध का प्रसंग भी आता है इसलिए १८वें काण्ड में ऋषेद की ऋचाएँ लेकर श्राद्ध का प्रतिपादन है और २०वें काण्ड में सोमपान का। १४वें काण्ड में विवाह के समय के मंत्र, शुभ-कामनाएँ तथा अन्य विवरण हैं। जैसा बताया जा चुका है अधर्ववेद में पद्य भी हैं और गद्य भी! ५ हिस्से पद्च में हैं, छठा हिस्सा गद्य में | विभिन्न वेदों के मंत्रों को सुरक्षित रखनें के लिए अलग-अलग क्रषियों को यह दायित्व दिया गया था कि बे इन्हें कण्ठस्ध करें और अगली पीढ़ियों को सिखाते जाएँ ताकि यह विशाल वाइमय अनन्तकाल तक जीवित रह सके। जिस प्रकार पैल ऋषि को ऋग्ेद का भार सौंपा गंया, जैमिनि को सामबेद का, वैशंपायन को यजुर्बेद का उसी प्रकार अधर्ववेद का सुमन्तु को। इन मुनियों ने बाद में वेदों की अलग-अलग शाखाएँ बनाकर अलग-अलग शिष्यों को उनका भार सौंप दिया। इन शाखाओं में से बहुत सी काल के धपेड़ों में न जाने कहाँ लुप्त हो गईं, केवल दो आज तक बची हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा धा नवधा आधर्वणो वेद: इससे ज्ञात होता है किस समय अधर्ववेद की ९ शाखाएँ थीं। आज तो बची खुची २ शाखाओं में से भी एक ही पूरी तरह जीबित है दूसरी का केबल नाम ही बचा है। यह शाखा है पिप्पलाद शाखा। अनेक वर्ष पूर्व पिप्पलाद संहिता कश्मौर में डॉ० बूलर को मिली धी जो भूर्ज पत्रों में लिखी धी। यह अब भी जम॑नी में सुरक्षित है। डॉ० राध ने इसे फोटो प्रक्रिया से छपवावा धा। जल की स्तुति में लिखा गया मंत्र शन्नोदेवीरभिष्टय जिसे आजकल पुरोहित लोग शनी का मंत्र बताकर शनी पीड़ित लोगों से जपवाते हैं, इस संहिता का पहला मंत्र है।
दूसती शाखा भारत में बहुत प्रचलित है जिसे शौनक शाखा कहते हैं। इसकी शौनक संहिता वर्षों से अधर्ववेदी ब्राह्मणों द्वारा पढ़ी पढ़ाई जाती है। इस वेद का सर्वाधिक प्रचार गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसमें शुद्ध उच्चारण और ऊँचे स्वर को प्राथमिकता दी जाती है। गाने या हाध हिलाने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती।
इस बेद के विवेचन से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रन्थ गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। मुण्डकोपनिषद् और प्रश्नोपनिषद् अधर्ववेद से सम्बन्धित उपनिषदें मानी गई हैं। देखा जाए तो इस वेद की शैली बहुत अनूठी और चित्ताकर्षक है। इसके पढ़ने से लगता है कि ‘एक विकसित सभ्यता और एक उन्नतिशील समाज लौकिक”अध्युदय और प्रगति के सर्वांगीण प्रयत्व में लगा हुआ है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नये नये तरीके और हथकण्डे सोचने में भी उसकी बुद्धि लग जाए तो आश्चर्य नहीं है। टोने-टोटके और दवाओं के नये नये प्रयोग इसी दिशा में किये गये प्रवत्न मालूम होते हैं। अधर्ववेद का कृषक गाय बैलों के संवर्द्ध और कृषि के विकास के तरीके सोचता है, युद्ध में विजय के रास्ते निकालता है, शत्रु द्वारा उखाड़ दिये जाने पर फिर जमने के उपाय निकालता है। ऐसे २९ कर्मों के बारे में मंत्र इस वेद में हैं। इनमें जहाँ जहाँ जादू टोने के संकेत मिलते हैं वे वास्तव में मार्जज या अभिमर्षण जिसे ‘मेसमैरिज्म’ या ‘हिपनोटिक सजेशन’ कहा जा सकता है और मानसोपचार जिसे ‘मैंटल-हीलिंगः कहा जा सकता है उसी दिशा में किये गये प्रयत्त लगते हैं। ये आदिवासियों के गण्डा ताबीज या ओझाओं के जादू टोने नहीं हैं, जैसा पाश्चात्य विद्वानों में से कुछ का कथन है। वस्तुत: इस बेद में पहली बार मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं की दृष्टि से मन्यु, मेधा, काम जैसी मानसिक वृत्तियों को देवता मानकर उन्हें सम्बोधित किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि मानसिक क्रियाकलापों के अन्दर पैठने की ललक बेद के क्रषि में जागृत हो गई धी। बड़ी अनूठी शैली में वे कहते हैं “हे ! अग्नि, तुझमें जो ताप है उससे मेरे शत्रु को जला और जो ऊर्जा है वह मुझे दे।’ इसी प्रकार चन्द्र, सूर्य, जल, सबके शुभ और अशुभ तत्वों में वह उल्लेख करता है। स्थापत्यकला, बस्निर्माणक्ला, शास्रों और आभूषणों के बनाने की कला, चिकित्सा विद्या, शरीर-विज्ञान, पाक-विद्या, पशुपालन, पक्षी-विद्या, इस प्रकार की असंख्य लौकिक विद्याएँ इस वेद का विषय हैं। ३०वें सूक्त में खानों से खनिज्ों को निकालकर तथा वनस्पतियों से औषधियों को निकालकर किस प्रकार मनुष्य के उपयोग में लाया जा सकता है इस पर लिखा गया है। ६४वें सूक्त में कौवे के आघात से बचने का तरीका और ६६वें आँधी से बचने का उपाय बताया गया है। इन सबसे लगता है कि अन्य वेदों में उच्चतर ज्ञान की विवेचना प्रमुख उद्देश्य होने के कारण जो व्यावहारिक और वैज्ञानिक बातें नहीं आ पायी थीं, उन सबका संकलन अधर्ववेद में करने का प्रयत्न किया गया है।