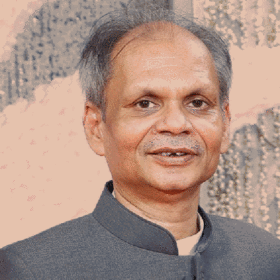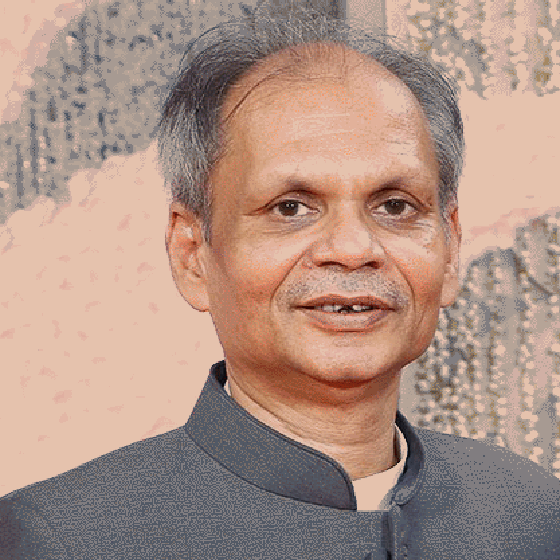वैदिक दर्शन

देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठठमाय कर्मणे । (बा.सं. 7-)
सविता देवता तुम लोगों को श्रेष्ठ कर्म में संलग्त करो।
जगत्, जीवन और व्यवहार- ये तीनों ैदिक दर्शन के प्रतिपाध पदार्थ हैं। सम्पूर्ण मानव-समाज इसका अधिकारी है। अभ्युदय और नि:श्रेयस प्रयोजन हैं। यजञज्ञान, देवताज्ञन और आत्मज्ञान– इनके लिए इस दर्शन में पारिभाषिक शब्द हैं– अधियज्ञ, अधिदेवत और अध्यात्म। जब लौकिक अभ्युदय के लिए. चर्मानुष्ठान करते हैं तब यज्ञज्ञान पुष्प हैं और देवताज्ञान फल। जब नि: श्रेयस प्राप्ति के लिए धर्मानुष्ठान करते हैं तब यज्ञ और देवता का ज्ञान पुष्प हो जाता है, आत्मज्ञान फल । सृष्टि पूर्व एक ही तत्त्व था। उसका नाम सूर्य, अग्नि या उषा था। वही एक इस ‘बिविध के रूप में प्रकट हुआ। एकत्व स्थिर रखते हुए. ही विविध हुआ।
ऋग्वेद का यह मंत्र दर्शनीय है–
एक एवास्निर्बहुधा समिद्ध:, एकः सूर्यों विश्वमनुप्रभूत: ।
‘एकैबोषा: सर्वमिर्द विभाति एक वा ‘इद विबभूब सर्वम् ॥ (8.58.2)
एक ही तत्त्व की दो विधाएं अवधारण की गई हैं- १. त्रिपाद 2. एकपाद्। त्रिपाद कहकर विश्व से परे होने का संकेत दिया गया है। एकपाद् का अर्थ है– विश्वरूपता और विश्वव्यापकता। बेद में इस तत्त्व के लिए ‘पुरुष’ शब्द का प्रयोग भी है। वह चतुष्पाद् है। पुरी में शयत करने के कारण या. उसे पूर्ण करने के कारण ‘ पुरुष! शब्द’की प्रवृत्ति है। उस समय पुरी क्या थी ?वह स्वधा थी, जो ‘स्व’ को धारण करे। वह तत्त्व शक्ति युक्त ‘धा–यह तात्पर्य है। विश्व सृष्टि के प्रारम्भ में वही स्वथा रूप जल समूह अर्थात् अपनी शक्ति को पृथक् करता है और भिन्न-भिन्न अपूकणिका में तेजोबिन्दु रूप से अपने को अभिव्यक्त करता है। श्रुति है– संभृतम् पृषदाज्यम् (वा.स॑. 3.66) अर्द्ध॑तारीनटेश्वर के समान अग्तीषोम या पुरुषस्वधा की आलिंगित दशा होती है। शतपथ श्रुति ने उसे “अर्धंवृगल’ कहा है। जैसे चने के भीतर दो दाल होती है परन्तु छिलके से ढकी रहती है, इसी प्रकार अबिन्दुओं के गर्भ में सृष्टि का बीज स्थिर रहता है, (संस्कृत-भाषा में ‘ अप्’ शब्द नित्य बहुवचनान्त हो होता है अर्थात् जल एक नहीं होता है, अनेक विन्दुओं का समूह होता है) वेदों में इस बिन्दु को रेणु भी कहते हैं। इन गतिशील जल समूहों में देबता स्थित थे और नृत्य करते थे। उनका परिभ्रमण चक्रवत् था। उनमें से एक बिन्दु या रेणु वेगाधिक्य से पृथक् हो गया-
चद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत ।
अत्रा वो नृत्यतामिव ती्रो रेणुरपायत ॥ (ऋ. 0.72.6)
यही पुरुष अनेक रूप धारण करने के लिए पहले त्रिवृत्त, त्रिणाभि अथवा एकनेमि सप्तारचक्र का रूप धारण करता है। उस सर्वश्रेष्ठ स्वधानुप्राणित परम पुरुष का यह एक अंश है।यह पुरुष इसी अंश से असंख्य अ्माण्डों के रूप में विवर्तित होता है। यही “सहसशीर्षा” पुरुष है; महाविराट् है। इसी से क्षुद्र और बिराद् का जन्म होता है। असंख्य ‘जगदण्डों में एक-एक अण्ड क्षुद्र विराद् है। प्रत्येक अण्ड में अगणित पिण्डरूप विराट हैं। वे भी क्षुद्र हैं। दोनों को ही दशाज़ुल पुरुष कहते हैं। प्रत्येक अण्ड का धिपुरुष
दया है। ब्रह्मा भी असंख्य हैं | ब्रह्माण्ड रूप यज्ञचक्र के अबर्तन में ब्रह्मा यजमान गृहपति हैं। वे तेज, रस एवं तपस्या हैं। काम, श्रम और तपस्या उनका स्वरूप है। मन से रेत या काम, वाणी से श्रम और प्राण से तप की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार यह ब्रह्मा मनोमय, बाडयय और प्राणमय हैं। मन सदसद्-विलक्षण है। ऋणषेद के नासदीय सूक्त में जो सत-असत् से विलक्षण का वर्णन है वह मत का ही है; देखिए, शतपथ ब्रह्माण (0.4.)। “ब्राणों का नाम ही असत् है। वे ऋषि भी कहलाते हैं” (शत. 6.0) : वाक् को सत् कहते । बाक् से भूतमात्रा अभिप्रेत हैं, प्राण से मुख्य प्राण, इद्ध और ऋषि, मन से बजापति। इनमें ब्रह्मा व्याप्त है। वही अपने शरीर के कम्पन से ऋषि, पितर और देवताओं को जन्म देता है। उनकी सहायता के लिए यज्ञ करता है। यह ब्रह्मा ही अकार, उकार, मकारात्मक प्रणव हैं; मन, प्राण एवं वाक् है। यह ब्रह्मा ही वाणी से ऑग्नि, पृथिवी प्राण से अन्तरिक्ष-वायु और मन से घुलोक-सूर्य का विभाजन करता है। महः, जनः, तप, सत्यम्, स्व: ये सब इसी के उत्कृष्टतर रूप हैं, सात लोक भी । ब्रह्मा का ‘शरोर सात कों
के अनुरोध से सप्त वितस्त अर्थात् साढ़े तीन हाथ है। दस दिशा और दश प्राणों की दृष्टि से दशाजुल है। क्षुद्र विराट प्रादेशमात्र है।
ऋग्वेद के (2.64.6) में यह मन्त्र है-
बि यस्तस्तम्भ षढ्िमा रजांसि ।
अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् ॥
श्रीमद्रागवत के ब्रह्म-स्तबन में ‘क्वाहं तम:’ इस श्लोक के ट्वारा इसी अर्थ का उपबृंहण या विवरण है । इस प्रकार सृष्टियज्ञ में ब्रह्मा लोकोपकार के लिए पूर्णतया आत्मदान करते हैं और अपने पिता सहख्रशीर्षा परम पुरुष नारायण को तृप्त करते हैं। साथ ही इस ब्रह्माण्ड को आत्मखरूप से ग्रहण करते हैं। सभी ब्रह्माण्डों में यह यज्ञ-चक्र प्रवृत्त हो रहा है। यह है अधिदैवत पक्ष।
अब अध्यात्म-पश्ष सुनिये। श्रुति का कहना है कि हम सब अमृत के पुत्र हैं । इस अर्थ के उपबृंहक वचन शास्त्रों में प्रसिद्ध है- न मानुषाच्छेष्ठतरं हि किल्धित्- मनुष्य से श्रेष्ठ दूसरा कुछ नहीं है । ब्राह्मण ग्रन्थ का कहना है- मनुष्य प्रजापति के निकटतर अर्थात् उससे मिलता-जुलता है। यह पिण्ड-श्रह्माण्ड की लघु प्रतिकृति है। इसमें भी आत्मा, देवता, ऋषि और पितरों को जो कि शरीर के संघटक तत्त्व हैं लेकर शतवार्षिक यज्ञ-चक्र का अनुष्ठान कर रहा है। यह जीवन भी स्वधांश से सम्परिष्कक्त होकर ही जीवित रहता है। स्वथा माने शक्ति । ऐतरेय ब्राह्मण में विदल संहित एव पुरुष: (4.22) कहा है।
मनुष्य के जीवन में स्वधा या शक्ति पत्नी है। यही अधिदेव का अनुकरण है। यह कोई अभिनय ही नहीं है, जीवन की पूर्णता भी है। यह शरीर ही जिणाभि, सत्तार, एकनेमि चक्र है। यह शतवार्थिक यज्ञ देवताओं का निवास है। यही देवताओं की पुरी अयोध्या है। अग्नि वाक् होकर मुख में प्रविष्ट हुआ। तैंतीस देवता इसी में रहते हैं । सात्त्क अतएब प्रकाशक, सुखदायक, सुन्दर, बलिष्ठ प्राण ही इसमें देवता हैं। जो इसको जान ले, उसके जीवन में दुःख का प्रसंग कहां है ?इस शरीर में यजमान या राजकुमार आत्मा है। वह ज्ञान एवं क्षमारूप बलशाली ऋषियों और देवताओं के साथ श्रेष्ठ कर्म रूप यज्ञ करता हुआ निवास करता है। यह अध्यात्म पक्ष है।
अब अधियज्ञ पक्ष को बिवृत करते हैं। यज्ञ अर्थात् सद॒व्यवहार, सदाचार। विद्वान् एक ही सत्य को विविध रूप से वर्णन करते हैं। एक सत्य की अनेक रूपों में, व्याप्ति ही सद्व्यवहार या सदाचार है। वही यज्ञ है। यज्ञस्तायते (वा.सं. 34.4) यह श्रुति है। इसका प्रचार-प्रसार होता है। जहां बहुत से लोग मिलें, परस्पर एक-दूसरे की पूजा करें, सत्कार करें, सबके लिए आत्मदान करें– अपनी वस्तुओं का दान करें। यज्ञ का यही व्यावहारिक अर्थ है। विधिपूर्वक अग्नि में हवन करना पूर्वोक्त अर्थ का अभिनय है। उसे भी करना चाहिए। “यज्ञ एक श्रेष्ठठम कर्म है’ (शत. 4.7..5) । उसका तात्पर्य है भोग, संग्रह एबं दान में त्याग की भावना ही मुख्य है। इसी यज्ञ बीज के अनेक अंकुर हैं। अपने को, समाज को, राष्ट्र को और जगत् को संतृप्त करना ही यज्ञ का रहस्य है। यह यज्ञ-क्रिया मानवता का चरम एवं परम उत्कर्ष है, प्रतिष्ठा हैं। यह दुःख की अन्त्येष्टि है। इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति सम हो जाती है। ईशावास्य का यह वचन जन-जन में प्रसिद्ध है- ‘इस यज्ञ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा करने पर मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता।’ “यज्ञ के लिए कर्म करने पर वह लीन हो जाता है, मनुष्य से लिप्त नहीं होता’ (गीता) । “जो अकेला भोजन करता है वह पाप का भोजन करता है (ऋ.) । सभी संप्रह दान के लिए ही होने चाहिए। ऋतुओं के संधिकाल में रोग होते हैं अत: डस समय यज्ञ करना चाहिए। हव॒नात्मक यज्ञ भी अपेक्षित हैं । महाविराट्, कुद्र एवं विराद् भी यज्ञ ही हैं| इनके स्वरूप को तत्त्वत: जानने के लिए यज्ञों का अभिनय किया जाता है। यह अधियज्ञ पक्ष है। संक्षेप में, यही वैदिक दर्शन है। यह आचरण के लिए है। इससे अभ्युदय और नि: श्रेयस-रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। यह बाद-विवाद या बुद्धि-व्यायाम के लिए नहीं है। अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है। हम अपने को भूमा सम्पन्न करेंगे–ऐसा जानना और इसी दृष्टि से आचरण करना वैदिक दर्शन है । वर्तमान युग के शिक्षितों ने विज्ञान, दर्शन और आचरण–इन तीनों को सर्वथा पृथक-पृथक असम्बद्ध मान लिया है। वैदिक-दर्शन इनका एक साथ बोध कराता है। अन्त में यह वैदिक प्रार्थना कीजिये-
आ ब्ह्मन् ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायतां आ राष्ट्र राजन्य: शूरःइषव्यो5तिव्याथी महारथो जायतां दोग्ध्ीं श्रेनुबॉढानड्बानाशु: सप्ति: पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न:ओषधय:ः पच्यत्तां योगेक्षमो न: कल्पताम्। (यजुर्वेद-22.22) देश में ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्थ्रो हों। क्षत्रिय शूर, लक्ष्यबेदी, निरोग एवं महारथी हों। गाय दुधारु हों। बैल निर्वाहक हों । घोड़े शीघ्रगामी हों। स्त्रियां पालन-पोषण की शक्ति से युक्त हों। युवा विजयी, पराक्रमी, सभ्य हों। हमारे घर-घर में ऐसे पुत्रर्त हों। आवश्यकता के अनुसार वर्षा हो। हमारी खेतीबाड़ी ‘फलती-फूलती-पकती रहे। जो हमारे पास नहीं है, वह मिले। जो है उसकी रक्षा हो।