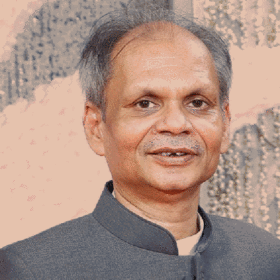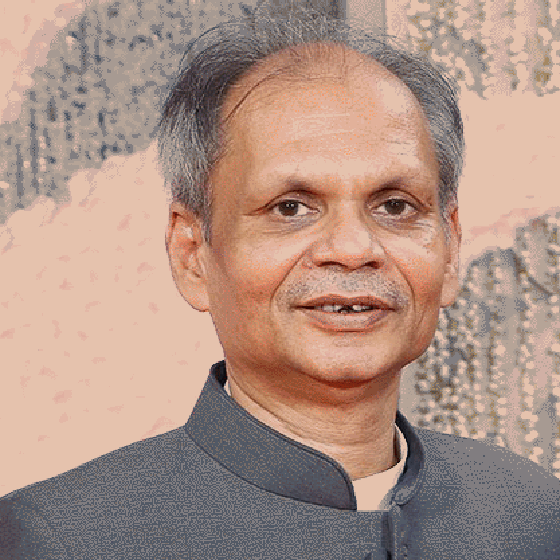वैदिक संस्कृति में ओंकार तत्त्व (Essence of OM in Vedic Culture)

अप्रिषोमौ पक्षाबोंकारः शिरों बिन्दुस््तु भेत्र मुखं रुद्ो रुद्राणी चरणौ बाहू कालश्चाप्रिश्चोभे पाश्वे भवतः।
विश्व एक ऊर्ध्व गतिमान उड़ते हुए पक्षी की तरह है।
ऑकार इसका शिशोबिलदु है, अगि और सोम इसके दो पंछ, ख और राणी इसके गेत्र एवं सुख, चरण एवं शुजाएँ काल, अग्नि इसके दोनों ओर व्यात्न है। यह परमहंस करोड़ों शूों के समान अकाशमान है एवं इससे ही वह सब ओरे से प्रटियूर्ण है।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो ओंकार के नाद तत्तवातुसार यह हमाती आकाशगंगा का एक अप्रतिम मॉडल है। वैदिकों का जगत् तात्विक दृष्टि से अग्निषोमात्मक है।
इसकी सर्पिल भुज्ञाओं में ऑकाए और अंकार का संगीत निज्तर गूँजता रहता है। अतः इसे ही शिरेबिनदु कहा गया है। ऊताए (ीपधए०त 50) ही केबस्थानीय रद है, उसके मुख या मुख्य भाग की विस्फोटक शक्ति हो रद्राणी है, चएण और भुजाएँ हो कालधर्मा बेगवान् गति, यहाँ अभ्नि और सोम से आप्लाबित करोड़ों सूर्य प्रकाशमान हैं। ओंकार का नादतत्व सम्पूर्ण वि में व्याप्त है-अण्ड से ब्रह्म तक, प्रत्येक तारे की द्रव्यात्मक रत्ता ओंकाएके परम संगीत की झंकार है; श्रुति का यहीं निर्वचन है-
…अथ खलु य उद्रथिः स प्रणवो यः प्रणव: स उद्गीध इत्यसौ वा आदित्य उद्गीध एप ग्रणवा
इत्येबं ह्वाहोद्रीं पणबाख्यं प्रणेतारं आारूपम्…. (मैत्रायप्युपनिषद् प्रया० ६-४)
यह आदित्य ही प्रणव है, यही इसका साम संगीत उद्रीष, वहीं अकाश स्वरूप सृष्ट है।
ओम का विश्वात्मक स्वरूप नाद है, विश्वातीत नादान्त अद्धण्ड ससस्वरूप है। नाद से ही विश्व का प्रथम बिन्दु उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे शिरोविन्दु कहा जाता है-नादात् बिन्दु समुदभव:।॥ ये नादात्मक ऊर्मियां (४0200) प्रलयग्रस्त विषुणात्मक द्रव्य को बिन्दुरूप में संगठित कर देती हैं-फलतः सम्पूर्ण द्रव्य बिन्दुभाव में घनीभूत हो उठता है यही विश्व का आदिअण्ड ((0०ञञआ० ८९४) है। इसका परम घनत्व नादतत्त के द्वारा महाविस्फोट क्रम (82-38॥8) में पहुँच कर विश्व-द्रव्य के रूप में अनन्त ब्रह्माण्ड चक्रों का विस्तार बन जाता है। नादांश या नादतत््व की ‘कलाएँ उसे विश्व के एक संगठित क्षेत्र ((॥7#60 4 ० एगांशटा5७) में बदल देती हैं। अण्ड-पिण्ड वाद के सिद्धान्तातुसास्न्यथा अण्डे तथा ब्रह्माण्डे-वह नाद क्रिया आदिअण्ड में, इसके पूर्व, महाविस्फोट रूप स्थिति में, ब्रह्मण्ड एवं प्राणपिण्ड की संस्वना में, सर्वत्र एकरूपा है-यही तो वैदिक ऋषियों का साम जाम का तत्व है। वहाँ उनकी स्व-स्व क्षेत्रगत अवस्थाओं के अतुप्तार इन नादकलाओं की भेद-भिन्नता-क्षेत्रतत आयाम परिणामी है। वही प्राण ऊर्मियों के रूप में प्राणपिण्ड का सृजन और उपसंहार करती है। हिंकाए से निधन तक यह तत्त्व उद्गीध विज्ञान में स्पष्ट किया गया है। प्राणकी तरह ही उसकी व्याहति आयामगत स्वरूप के अनुसार तद्दत्, _आदिअण्ड तक परिव्याप्त है। वेद- दान्त-योग- तन्त्र-पुराण ओम् के विश्व और विश्वातीत स्वरूप को अली-भाँति स्पष्ट करते हैं। ओम् में दो वर्ण और चार मात्राएँ हैं। इन चाऐँ मात्राओं के ‘स्पन्द’ (?540॥) से समग्र पदार्थों की संरचना होती है। ऊर्मिधाराएँ-जो धारण करती हैं वही धाराएँ हैं। धारा शब्द का यही “धा’ धातु से अर्थ निष्त्न होता है-नाद के स्पन्द की मात्रा में ही विश्वद्रव्य का समायोजन अवधारित होता है। दधाराएँ या स्पन््दमात्रक में तीन क्रियाएँ एक साथ होती रहती हैं-धारण-नवोत्पादन-व्यापन। इसके समायोजन से ही सृष्टि का आदिअण्ड हिण्यगर्भ उत्पन्न होता है। आगम ग्रन्थों के अनुसार नादतत्व का कलात्मक स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है।
अ्धम नाद की तीन कलाएँ व्यक्त होती हैं-अ-उ-म् । इसका एकीभूत स्वरूप ही ओकार है। “अ’ के नादशक्तिजन्य स्वरूप का नाम ब्रह्मा है, इसकी आठ उपकलाएँ हैं-(१) सिद्धि, (२) ऋद्धि, (३) च्युति, (४) लक्ष्मी, (५) मेधा, (६) कात्ति, (७) धृति, (८) सुधा। ‘उ’ का नादशक्तिजन्य स्वरूप विष्णु नाम का तत्त्व है, जिसकी तेरह उपकलाएँ हैं-(१) सजा, (२) रक्षा, (३) रति, (४) पाल्या, (५) म्या, (६) बुद्धि, (७) माया, (८) नाड़ी, (९) भ्रामिणी, (१०) मोहिनी, (११) तृष्णा, (१२) मति और (१३) क्रिया। “म्* के शब्दजन्य नाद का नाम रुद्र है- जिसकी सात उपकलाएँ हैं-(१) तमोमोहा, (२) सुधा, (३) निद्रा, (४) मृत्यु, (५) माया, (६) मया और (७) जड़ा। इनके अंशांश के सम्मिश्रण से ये असंख्य हो जाती हैं। महानाद का ऊर्ध्वगमन ही नादतत्त्व ‘का-ओंकार-अ-उ-म् स्वरूप है, जो विश्व की संस्चना में ८६१३+७-२८ कलाओं से समूहित जिस नादाण्ड का निर्माण करता है-वही हिरण्यगर्भ का आदि महाण्ड है, जिससे काल और कला का आश्रय लेकर ये अनन्त ब्रह्माण्ड चक्र बहिर्भूत होते रहते हैं। मादाण्ड के बल-वेग से विस्फोटित द्रव्ययाशि में जिन कलातत्त्वों का मिश्रण प्रधान होता है, वैसा ही ब्रह्माण्ड और वैसा ही उसकी ‘जीवन-धाद के विकास और विस्तार हो जाता है।
बिन्दु ही सिन्धु बन जाता है-आदि बिन्दु का पस्मकण ही विश्व संस्चना का हेतुभूत है। उपासना का परमबिन्दु ओंकार है- प्रणबों ह्वापरं ब्रह्म प्रणवश्च पर: स्मृत:। (गौड्पाद कारिका १.२५)
कह्ली विस्वातीत एसत्रह्ा का स्वरूप-वली प्रद्नह्व है, वही अपखहा-
श्रुतिभगवती का यही मन्तव्य है- त॑ बा एतमात्मान॑ परम॑ ब्रह्मोक्वरम्…। (श्रीनृसिंहोत्तततापनीयोपनिषद् खण्ड ४) प्रणव से ही प्रकृति का स्वरूप निर्मित होता है- प्रणवात्प्रकृतिरीति बदन्ति ब्रह्मवादिन:। (श्रीरामोत्तततापनीयोपनिषद् ४) इसीलिए कठ श्रुति इसे उपासकों की कामधेनु कहती है-
‘एतद्बेवाक्षरं ब्रह्म होतद्धायरेवाक्षरं परम्।
‘एतद्ध्बेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्।! (कठोपनिषद् १-२-१६)
बह ओम् एक अक्षर है, यही ब्रह्म है, यही सबसे परे है, इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ भी चाहता है, उस्ते वह आप हो जाता है। गणव ही प्राणक्रप हो जाता है, अतः आपत्त्व का साररूप अपव के अधीन है।
अथर्वण श्रुति का कथन है- प्रणव: सर्वाश्ग्राणान् प्रणामयति नमयति। (अधथर्वशिखोपनिषद्)
प्राण का ऊर्ध्वममन ओम् के आश्रय से होता है, यही श्रीमदूभगवद्गीता में भगवान् वासुदेव का स्पष्ट कथन है-
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहज्मामनुस्मरन् ।
य; प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्॥| गीता-८-१३)
ब्रह्म पद का बाचक प्रणव या ओम् है, यही अभिमत योग दर्शन का भी है-तस्यवाचक: प्रणव: ॥| (योगदर्शन १-२७)। भागवत के अनुसार वह परमात्मा का साक्षात् वाचक एवं सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद् और वेदों का सनातन बीज है। ओंकार के अकारादि तीन वर्ण ही सत्य, रज, तम इन तीन गुणों, ्रकू-यजुः-साम इन तीन नाम, भूः-भुवः-स्वः इन तीन अर्थ और जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति-इन तीनों वृत्तियों का रूप में तीन-तीन की संख्या वाले स्वरूप को धारण कर्ता है-
स्वधाम्नों ब्रह्मण: साक्षाद् वाचक: परमात्मन:। स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीज॑ सनातनम्॥ तस्य ह्ासंख्यो वर्णा अकागाद्या भूगूहृह। धार्यन्ते यैख्नयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः॥ (भागवत १२-६-४१,४२)
बैदिक वाड्मय में ओम् पर प्रभूत विचार किया गया है। छान््दोग्य उपनिषद् का विषय-प्रवर्तन ही ओम् की उद्गीध उपासना से होता है। “गोपध ब्राह्मण’ के अनुसार यह पद ड्विवर्ण और चार मात्रा वाला है। छान््दोग्य और माण्डूक्य श्रुतियाँ इसका व्याख्यान
विस्तार से करती हैं, पर माण्डूक्योपनिषद् के अनुसार यह पद तीन मात्रा वाला है। आत्मा को वहाँ चतुष्पातू-सोध्यमात्मा चतुष्पात्
कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार चार मात्राएँ हैं। ओम् के प्रकृति-प्रत्यय को लेकर वहाँ अनेक प्रश्न किये गये हैं, जो इसके महत्त्व को स्पष्ट करते हैं। गोषथ ब्राह्मण का विषय-प्रवर्तन इस मन्त्र से होता है-ओरेम् ब्रह्म ह वा इदमप्र आसीत्-ओम् ब्रह्म ही
निश्चित रूप से सर्वप्रथम था। उसने तप किया-अर्धात् तोपशक्ति को उत्पन्न किया, इससे ही सारे पदार्थों की सृष्टि होती है। ओम
जाद है-इसके तरंग प्रकम्प से उत्पन्न ताप के विभिन्न मात्रक ही विभिन्न जागतिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। वहाँ श्रम और तप
पद का प्रयोग है-
तदभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत्… (गोपथ ब्रा० पू० भा० कं० १-१)
उसे सत्र ओर से अम किया; सब ओर से तप किया, भली-भाँति तप किया।
आपेपालड्कार की सीमा में देखा जाय तो-“नाद’ का श्रम-उसका ग्रका्पन है (050॥॥ं0०7), तपत् समतपत्-न्यह उसकी मात्रा के ग्रकम्प से जन्य ताप शक्ति का संवर्धन है । नाद के तरंग प्रकम्प से ही विभिन्न पदार्थों का निर्माण और उनका अवधारण होता है-तस्मात् धारा अभवस्तद् धापणां धार वाह प्रियते-(गोपथ ब्रा० पू० भा० कं० ६-२)। वाद से होने वाले ताप और दबाव से जीबन और जगत् के निर्माण का उल्लेख है। इससे आगे की कण्डिका में देव-प्राण, ऋषि-प्राण और प्रजापति-प्राण की रचना का वर्णन है। “ओम्’ यह महाव्याहति है इससे ही पुरुष के सम्पूर्ण पुरुषार्थ का स्वरूप प्रकट होता है। इसके ही ताप और दबाव या चाप से तौन लोक, तीन बेद, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि पाँच तत्व अस्तित्व में आते हैं। इससे ही तीन व्याइतियाँ-भू:- सुब:-स्व: हैं, जिनका क्रमशः ऋचेद, यजुर्वेद और सामचेद से सम्बन्ध है। ‘गोपध ब्राह्मण” की आठ कण्डिकाओं का सार-संक्षेप यही है-विश्व के आधारभूत भूनु और अंगिततत्त ओंकार से ही प्रकट होते है | तेरहवीं कश्डिका में यज्ञ संस्था की संस्चना का कथन ह-अप्नि होता बन गया, वायु अध्व्, सूर्य उद्ाता, चत्मा ब्रह्मा, याजक या वजमान पर्जन्य । यहाँ उद्ान या उद्दीथ का सम्बन्ध आदित्य से है, अतः इससे ही साम का वितान होता है, इसलिए उद्रीध सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है-उससे ही साम का स्वरूप व्यक्त होता
है।
ब्रह्मा के प्रकट होने पर उसके समक्ष विश्व-संरचना की समस्या उत्पन्न होती है-उसने सर्वप्रधम दो बर्ण और चार मात्रा वाले ओम अक्षर को देखा-जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्विकार ब्रह्म है, उसमें ही ब्रह्म की व्याहृति और उसका दैवत-तत्त्व विद्यमान
था। उससे ही उसने सब कामनाओं, सर्वलोक, सम्पूर्ण देवसंस्था, चार बेद, उपबेद आदि प्रस्तुत कर (दिये थे। यहाँ मूल रूप से संरचना के दो विभाग हैं-ज्ञानसत्तात्मक एवं वस्तुसत्तात्मक, प्रथम का सम्बन्ध वेद-उपबेद आदि से है, दूसरा संसार और उसके द्रव्यभूत पदार्थ ।
ओम की प्रधम मात्रा “अ’ से पृथ्वी, अग्नि, औषधि, वनस्पति, ऋण, भू: व्याहति, गायत्री छन््द, त्रिवृ्त स्तोम, पूर्व दिशा, यसन््त ऋतु, आत्मस्वरूपा वाक्, स्सेन्द्रिय का निर्माण होता है। द्वितीय स्वर मात्रा +उ’ से अन्तरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, सर्वव्यापक भुवः नाम वाली ब्याहति, त्रैष्ठभ छन्द, पशदश स्तोम, पश्चिम दिशा, ग्रीष्म ऋतु, गराण, गन्ध, ब्रणेन्द्रिय प्रकट होती है। तृतीय मात्रा ‘ओ’ से दिवस, आदित्य, सामवेद, आनन्दस्वरूपा स्व: नाम व्याहति, जगती छन्द, सप्तदश स्तोम, उत्तर दिशा, वर्षा ऋतु, ज्योति, नेत्र अस्तित्व में आते हैं। ‘उ’ के सम्प्रसारण से व्यक्त होने वाली “ब” कार मात्रा से जल, चन्द्रमा, नक्षत्र, अधर्वबेद, अंगिरस, अनुष्ठप
छन््द, एकविंश स्तोम, दक्षिण दिशा, शरद ऋतु, मन, ज्ञान-ज्ञेय आदि पदार्थ ब्रह्मा ने बनाये। “म’ कार की श्रुति से इतिहास-पुराण, बाकोवाक्य, गाथा, नाराशंसी, शिक्षा, उपनिषद्, अनेक व्याइतियाँ, वीणा आदि वाद्य यन्र, अनेक प्रकार के वैदिक एवं लौकिक छन्द, अनेक स्तोम, ऊपर-नीचे की दिशाएँ, हेमन्त-शिशिर ऋतु, कर्मेन्द्रिय आदि का निर्माण सम्पन्न हुआ।
ओम् को एक अक्षर वाली क्रचा कहा गया है, जो ब्रह्मा के तप कल्ने के पूर्व ही प्रकट हो गई थी-सैपैकाक्षणक्रग् दह्णस्तपसोओ प्रा्बभूव…. (कं० १-२२) इसकी प्रथम मात्रा का रंग लाल है-न्रह्मा देवता; दूसरी मात्रा का रंग काला-विष्यु अधिदेवता; तीसरी का रंग पीला एवं इसके देवता ऐशान हैं, जो आधी के साथ चतुर्थ मात्रा है, उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक की तरह पस्म उज्वल-यह सर्वदेवात्मक है। ओंकार चारों वेदों का देवता कहा गया है-देवता ओडकारो वेदानाम्। व्याकरण की दृष्टि से ओम् पद की धातु-‘आप्त:” है, इसके दो प्रकार के निर्वचन प्राप्त है-*अबतिम्!-रक्षा करना, दूसग-‘आप्त! अर्थात् व्याप्त होना। दोनों ही अर्थ यहाँ व्युत्पन्न होते हैं-यह सबकी रक्षा करता है इसलिए. *अवति’-ओंकार ही सर्वत्र व्याप्त है, अतः “आप्नोति’ अर्थ भी समीचीन है। निपातों की दृष्टि से व्याकरण इसे उदात्त मानता है। यह दो वर्ण और एक अक्षर वाला है। इसका छन््द गायत्री है, देवताओं कीगायत्री एक अक्षरवाली स्वेतवर्णा कही गई है-गायत्रं हि छन््दों गायत्री बै देवानामेकाक्षरा श्वेतवर्णा च व्याख्याता (कण्डिका १-
२७) | यहाँ प्रकृति-प्रत्यय की दृष्टि से ओंकार के व्याकरण पर ३६ प्रश्न किये गये हैं।
ओम् को ही आत्मज्ञान का अधिकरण, ओषध एवं आत्मा का मोक्षमुख कहा गया है- अध्यात्ममात्मभैषज्यमात्मकैवल्यमोंकार:
(कण्डिका १-३०)। ‘आत्मा’ शब्द का व्याकरण इस प्रकार है-‘आ’-सर्वत्र अर्थात् चारों ओर, ‘अत्’+“मन्’> पहुँचने वाला,
जो सर्वत्र पहुँच कर व्याप्त हो गया है, या जो सर्वत्र व्यापक है वह “आत्मन्’ तत्त्व है। आत्मा में ‘उक्थ’, ‘ब्रह्म” और ‘साम’ तीनों
ही विद्यमान हैं-अर्थात् जो उठा हुआ है, जिसमें निवास करता है, जो उत्पन्न बस्तु में समान रूप से व्याप्त रहता है, वही उसका
आत्पतत्त्व कहा जाता है। हम पहले मन-प्राण और वाक् का उल्लेख कर आए हैं-मन ही वहाँ कामना या इच्छा रूप है, प्राण की
क्रिया ही तप है, वाक् से होने वाली क्रिया श्रम। कामना या इच्छा मन का कर्म है, शरीर में होने वाली चेष्टारूप क्रिया प्राण एवं
उसके पाँच तत्वों का कर्म श्रम। मन-प्राण-वाक् के एकात्म सम्बन्ध से उत्पन्न तत्त्व का नाम प्रजापति है, जितने पदार्थ उतने ही सारभूत
स्वरूप प्रजापति कहे जाते हैं। अतः पदार्थमात्र का अपना-अपना एक प्रजापति है, इनकी समष्टि विश्व । प्रत्येक प्रजापति ओम् कहा
जाता है, इस अक्षर में जो ध्वनि है-कर्णेन्द्रिय जिसके खण्डों का पृथक्-पृथक् अतुभव करती है-वह वाक् है। इसमें जो स्वर का
भाग है-जो वर्ण में उतार-चढ़ाव और समानता की प्रतीति-अर्थात् उदात्त-अतुदात्त-स्वरित, यह प्राणतत््व का अंश है। ओम् पद
के उच्चारण काल में जहाँ हम किसी प्रकार के अर्थ का बोध प्राप्त करते हैं वह मन का भाग है। यह बोध ग्रत्येक शब्दमात्र में विद्यमान
है, इसलिए प्रत्येक अर्थवान् शब्द प्रजापति है पर *ओम्’ अक्षर में इन तीन धर्मों की विशेष अभिव्यक्ति को लक्ष्य में रखकर उसे
विशेषतया प्रजापति कहा गया है, अन्य में गौण भाव के कारण उनकी चर्चा नहीं।
ओम् के उच्चारण से विशेष प्रकार के साम की अभिव्यक्ति होती है, उद्रीथ विज्ञान इसके स्वरूप को भली-भाँति स्पष्ट करता
है। साम के प्रस्ताव तो अनेक हैं-पर निधन एक ही है। अनेक स्थान से प्रवाहित होने वाली सोम धागएँ अन्त में एक ही केद्र में
पहुँचती हैं, जिस प्रकार नदियों के उद्गमस्थल या प्रस्ताव अनेक हैं-पर निधन-जहाँ सब एकाकार हो जाती हैं, बह समुद्र एक ही
है। प्रस्ताव का अर्थ है उत्स या उदगमभूमि-निदान उद्गत की मिलन-भूमि है। जिस स्थान से सोम की गति अपने केन्द्र की ओर
‘गमन करती है-वह प्रस्ताव है, जहाँ जाकर वह समाप्त होती है वही निधन है। वेद के अनुसार प्राण सामरूप है, अर्चि ही
क्रकू-इसीलिए क्रचा पर आरूढ़ साम गाया जाता है-कऋच्यध्यूढं साम गीयते-यही वैदिक सिद्धान्त है। अतः महान् वैयाकरण
आचार्यप्रवर दुर्ग के वचन द्वारा हम यहाँ ओंकार की महान् महिमा को बार-बार प्रणाम करते हैं-
कार बिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिन:।
कामदं मोक्षदं देवमोड्काराय नमो नमः ।॥