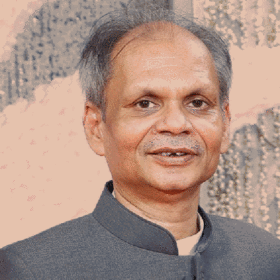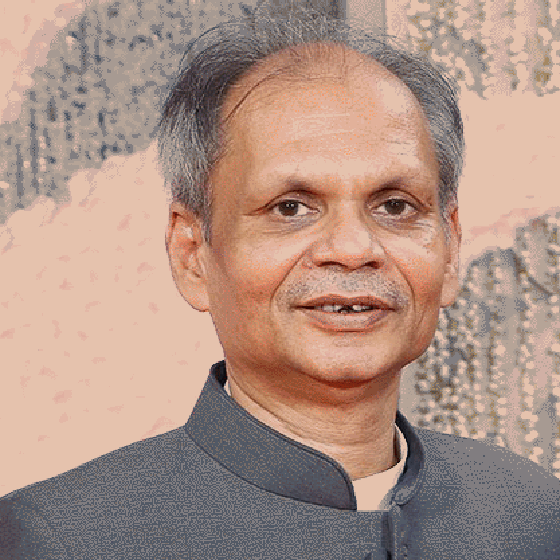Toward Poetry (कविता की ओर)

आत्मा की श्रादि प्रेरणा ह। आत्मा की गूढ जौर छिपी हुई सौदय राशि का भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही ‘कविता ह। जिस समय आत्मा का व्यापक सौन्दय निखर उठता हू, उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम हो जाता हू । उस समय क्षण क्षण म मे और ‘सब’ में विषयय होता ह। ‘मे” चिर तन भावनाओ में सबका रूप धारण करता ह और सब’ भायना के किसी विदेष वष्टि बिदु मे ‘मै’ में आकर सकु चित हो जाता हू । तब व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अबाधरूप से प्रवाहित होने लगती ह जोर समस्त सृष्टि का सगीत एक कण मे स्पन्दित होने लगता है। जिस दैवी क्षण में कवि अपने को इस असीम प्रकृति मे विलीन कर. देता ह, उस क्षण में सृष्टि के समस्त रहस्य उसकी वाणी में फूट पडतें ह। वह अपनी भावनाओ के भीतर किसी प्रजापति को देखता ह, जो क्षण क्षण में सृष्टि का निमाण और विनाश करता ह । रूप और व्वनिया साकार और निराकार होती है और दश्य और अदश्य उसे अपने सगीत से ओत प्रोत कर देते है । समस्त जगत हृदय में गतिशीलता भर कर तिरोहित हो जाता है, उसी गतिशीरूता का नाम कविता’ है।
यह कविता की व्यारया हु, परिभाषा नही । परिभाषा के लिए हमे काव्य से श्रेष्ठतर सौ दय कोटि की कल्पना करनी पडेगी और उस कोटि के अ तगत काव्य के समकक्ष अय रूपो से काव्य की विशेषता स्पष्ट करनी होगी । कठिनाई यह ह कि काव्य के ऊपर कोई ऐसी सो दय कोटि ह ही नही। काव्य ही अपने व्यापक रूप मे अनेक सौन्दय कोटिया निर्धारित करता हू ओर जब’ का०्य अपने उदात्त रूप में ब्रह्मान द के समकक्ष होता ह तब जिस प्रकार ब्रह्म की परिभाषा देना कठित है, उसी प्रकार काव्य की परिभाषा भी देना कठिन होता है । केनोपनिपद् के द्वितीय खण्ड में ब्रह्म-ज्ञान की अनिवचनीयता का उल्लेख ह
नाह मये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यो नस्तद्वेद तद्देद मो न वेदेति वेद च ।
( केनोपतिषद–ह्वितीय खड, इलोक २, ३ )
यस्यथामत तस्य मत मत यस्य न वेद से ।अविज्ञात विजानता बिज्ञोप्तभजिजनित भिं ॥
( न तो मै यह मानता हूँ कि मै ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और न यही समझता हैं कि मै उसे नही जानता, अत मै उस्ते जानता भी हूँ और नही भी जानता। जो उसे ‘न तो नही जानता और न जानता ही हूँ इस भाति जानता ह, वही जानता ह )
इसी भाति जिसको ब्रह्म ज्ञात नही ह, उसी को ज्ञात ह, ओर जिसको ज्ञात है, वह उसे अज्ञात ह, क्योकि वह जानने वालों को बिना जाना हुआ हूं और न जानने वालो का जाना हुआ है। इस प्रकार कविता भी पूण रूप से जानी जा सकती ह, इसम सन्दह ह । इसी लिए कविता की ध्याएया तो हो सकती ह, उसकी परिभाषा दना एफ अनविफार चेष्टा है ।
साहित्य के अन्य रूपो की अपेक्षा कविता की अभिव्यक्ति सभवत सवप्रयम हुई । यह साहित्य कानन की प्रथम कलिका ह, जिसकी सुरभि उत्तरोत्तर अधिक आह्वादमयी हाती गई । उसी सुरभि के आकषण में साहित्य के अय रूपो को मुकुलित हाने की भूमिका प्राप्त हुई होगी। कविता के इतिहास में प्रथम कविता मह॒षि बाल्मीकि के कण्ठ से क्रोतत बन के विपाद से नत्र की अश्रु धारा के साथ निकली कही जाती ह किन्तु कविता को सुष्टि उस समय आरभ हा गई होगी जब उल्छास या करुणा, आकषण और आत्म समपण की भावना ने हृदय में ऐसी विह्न॒लता भर दी होगी, जिसे हृदय अपनी भाव सीमा में सम्हार्ष न सका होगा ओर काव्य का अमत भाषा में छछक पडा होगा । महाकवि तुलसी ने कविता के आविर्भाव के सम्ब – में रामचरितमानस में कुछ
सु दर पक्तिया लिखी हँ
हृदय सि धु, मति सीप समाना,
रामचरितमानस
स्वाति सारदा कहृहि सुजाना ।
जो बरसइ बर बारि बिचारू,
होइ कवित मुक्तामनि चारू।
हृदय के सिन्धु मे मति सीप के समान हू, काव्य की प्रतिभा या सरस्वती स्वाति नक्षत के समान ह । इस अवसर पर यदि सुदर विचारों का जल बरस जाय तो भावना की सीपी मे कविता का मोती निर्मित हो जाय । सीप मे मोती का निमाण एक अवसर विशेष की बात ह। यदि सौभाग्य से ऐसा अवसर आ जाय, तभी कविता की सष्टि हां सकती ह। श्रेष्ठ कविता भी सयोग से ही बनती हू, और वह भी प्रतिभा के आलोक से सभव होता हु ।
कविता जीवन का निर्बाव और अक्ृत्रिम सो दय-बोब है, उसके द्वारा मानत्र ऐसे अनवरत ओर अविरल आनाद का अनुभव करता ह जो समय की गति से वूमिरू नही हांता । इसमें पूव चिन्तन की अपेक्षा नही ह। जिस प्रकार हास्य और रुदन की प्रक्रिया किसी नियम पर आधारित नही हू, हसी की कली प्रस्फुटित होने के पूृव यह नही सोचती कि उसे किस प्रकार से प्रस्फुटित होना हू, जिस प्रकार रुदन के मोती किसी निश्चित सरया में नहीं अरते, उसी प्रकार कविता प्रयास पूवक निर्मित नही होती । वह आनद को धारा में पृष्प की भाँति लहरा की गोद में विकसित होती ह ।
प्राचीन आचार्यो मं भरत, दण्डी, रुद्रठ, वामन, आनादवद्धन, भोज, मम्मठ, वास्भट्ट, जयदेव, विश्ववाथ, पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के रूप को परवखने की चेष्टा विवि दष्टि कोणों से की ह। आचाय भरत ने रस को, दण्डी ने सक्षिप्स वाक्य को, रुद्रठ मे शब्द और उसमे निहित अथ के युग्म को, वामन ने रूलित पद रीति को, आन दवद्धन ने ध्वनिमयी अथ निष्पत्ति को, भोज ने निर्दोष अलकारमय अथ को, मम्मट ने शब्द और अथ की सयोजना को, वाग्भट्ट ने दोषरहित शब्द को, जयदेव ने रसमयी शब्द-योजना को विश्वनाथ ने रसात्मक वावय को और पण्डितराज जग नाथ ने रस से पूण अथ वणन को काव्य माना ।
काव्य की इस नाना दष्टिमयी विवेचना में तीन तत्त्व निहित ज्ञात होते हैं —
१ रस की अनिवचनीय अलौकिक भाव भूमि ।
२ शब्द और अथ का ललित युग्म ।
३ चमत्कार उत्पन करने वाली व्यज्ञना ।
यह कहा जा सकता ह कि अनुभूति के स्तर पर शब्द और अथ का तादात्म्य उपस्थित होने पर ही रस को निष्पत्ति होती ह। जिस अनुपात में यह तादातम्य होगा उसी अनुपात में रस जनित जानद की सष्टि होगी, कठिनाई केवल तादात्म्य उपस्थित करने मे ह। यह स्पष्ट हु कि अनुभूति जगत इतना विस्तत है कि उसकी अभिव्यक्ति कभी शब्द द्वारा हो सकेगी, इसमे स देह है । मन की गति जितनी शीघ्रता स अथ के विराट विश्व मे प्रवेश करती ह, उतनी शीघ्रता से भाषा अपना स्थूछ उपादान प्रस्तुत नही कर सकती । इस समस्या का अनुभव करते हुए मैने एक स्थान पर लिखा था
अतजगत अपनी सम्पूण परिधि दब्दो द्वारा व्यक्त नही कर सकता। भावनाएँ अपनी गहराई मे अभाह है और शब्द किनारे पर बैठे हुए पथिक है जो केवल लहर गिनना जानते ह। जिस साधक में अपने शब्दों को अथ में डुबानें की जितनी अधिक सहज क्षमता होगी उतनी ही गहरी रसानुभूति काव्य के माध्यम से हो सकेगी ।